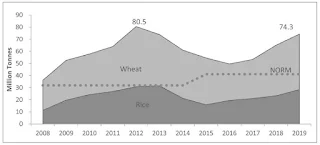(भारत में खाद्य उत्पादन और उपभोग की प्रवृत्ति, खाद्य सुरक्षा की
समस्याएँ, भंडारण की समस्याएँ और मुद्दे, उपलब्धि, वितरण, आयात और निर्यात, सरकारी
नीतियाँ, योजनाएँ और कार्यक्रम जैसे पी.डी.ए., आई.सी.डी.एस. और मध्याह्न भोजन आदि)
खाद्य सुरक्षा की अवधारणा
खाद्य
सुरक्षा की परिभाषा "सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर एक सक्रिय, स्वस्थ
जीवन के लिए पर्याप्त भोजन की उपलब्धि के रूप मेंक्षहै"। किन्तु खाद्य एवं कृषि संस्था का अर्थ (Food and Agriculture
Organisation) ने खाद्य सुरक्षा “सभी व्यक्तियों को सभी समय पर उनके लिए आवश्यक बुनियादी भोजन के लिए भौतिक एवं आर्थिक दोनों रूपक्षमें उपलब्धि के आश्वासन के रूप में की है"।
आम
तौर पर खाद्य सुरक्षा की अवधारणा की चर्चा समग्र जनसंख्या के लिए खाद्यान्नों की
न्यूनतम मात्रा उपलब्ध कराने के रूप में की जाती है। इस दृष्टि से यह अवधारणा
संकुचित है, परन्तु एक गतिशील और विकासमान अर्थव्यवस्था में खाद्य सुरक्षा की
अवधारणा समाज द्वारा विकास की अवस्था में परिवर्तन के साथ तब्दील होती रहती है।
खाद्य समस्या का स्वरूप
अध्ययन
की सुविधा के लिए खाद्य समस्या के चार पहलू माने जाते हैं
- मात्रात्मक (Quantitative) गुणात्मक (Qualitative), प्रशासनिक (Administrative) और
आर्थिक (Economic)। इन्हें निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है।
मात्रात्मक पहलू
इसका
सम्बन्ध खाद्यान्नों की मांग व पूर्ति से होता है। सामान्यतः खाद्य सामग्री का
उपलब्ध परिमाण प्रायः मांग से कम रहा है, अत: खाद्य समस्या एक अल्पकालीन संकट नहीं
अपितु दीर्घकालीन समस्या मानी जाती है। इस समस्या का समाधान उत्पादन बढ़ाकर किया
जा सकता है। लेकिन वर्ष प्रति वर्ष उत्पादन में बहुत घट बढ़ होती रही जिससे कभी-कभी
समस्या अधिक गंभीर हो जाती है और आयातों का सहारा लेना पड़ जाता है। उदाहरण के तौर
पर 1966 में खाद्यान्नों का विशुद्ध आयात एक करोड़ तीन लाख टन हुआ था जो योजनाकाल
में सर्वाधिक माना गया है। इसके अतिरिक्त योजना काल में खाद्यान्नों के उत्पादन
में वृद्धि होने से भारतीय अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर कही जाने लगी है। लेकिन यह
स्थायी किस्म की नहीं हुई है। मात्रात्मक पहलू को दृष्टि से पहले की तुलना में
स्थिति बेहतर अवश्य है। दीर्घकाल तक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए इनका
उत्पादन बढ़ाने के साथ जनसंख्या वृद्धि पर भी प्रभावपूर्ण नियंत्रण करना होगा।
गुणात्मक पहलू
अधिकतर
भारतीय जो भोजन करते हैं उसमें पोषक तत्वों की बड़ी कमी रहती है। भोजन में
प्रोटीन, विटामिन और खनिज पदार्थों का अभाव बना रहता है। जिससे श्रमिक वर्ग की
कार्यकुशलता पर भी बुरा असर पड़ता है। अतः स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि खाद्य
समस्या का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि देश के सभी नागरिकों को संतुलित एवं पौष्टिक
आहार मिलना चाहिए। प्रो. अमर्त्य सेन के अनुसार भारत में ग्रामीण जनता का लगभग एक
तिहाई भाग सदैव भूख एवं कुपोषण का शिकार रहता है।
प्रशासनिक पहलू
इसका
सम्बन्ध वितरण पक्ष से होता है न कि उत्पादन पक्ष से। सामान्यतः यह संभव है कि
खाद्यान्नों का उत्पादन तो बढ़ जाए लेकिन वितरण व्यवस्था के दोषपूर्ण होने से
खाद्य समस्या निरन्तर बनी रहती है।
आर्थिक पहलू
भारत
के कई बार यह देखा जाता है कि महंगे अनाज को क्रय करने के लिए लोगों के पास आवश्यक
क्रय शक्ति का अभाव रहता है अर्थात इस पहलू का सम्बन्ध जनता की गरीबी तथा
खाद्यान्नों के ऊँचे भावों से होता है।
खाद्य उपयोग प्रकृति एवं खाद्य समस्या के कारण
पिछले
वर्षों में भारत में खाद्य स्थिति में सुधार हुआ है। देश को खाद्यान्नों में आत्म
निर्भर माना जाने लगा है। लेकिन खाद्य समस्या को अभी भी समाप्त हुआ नहीं माना जा
सकता है। अतः खाद्य समस्या हल करने के लिए यह जानना आवश्यक है कि किन कारणों ने
इसे जन्म दिया है और इतने लम्बे समय तक किन कारणों ने इसके समाधान में कठिनाई
उपस्थित की है। दीर्घकालीन दृष्टि से इस समस्या के निम्न कारण उत्तरदायी माने जा
सकते हैं।
भारत में वस्तुओं की मांग
सामान्यतः
वस्तुओं की माँग बड़े पैमाने पर बढ़ती रही है। मांग में यह वृद्धि मुख्यतः निम्न
कारणों से हुई।
(1) जनसंख्या में तीव्र वृद्धि-जनसंख्या वृद्धि व आय
में वृद्धि से खाद्यान्नों की मांग बढ़ रही है। अकाल व सूखे के
दौरान देश में खाद्यान्नों की कमी महसूस की जाती है अत: स्पष्ट है कि जनसंख्या की
अत्यधिक वृद्धि खाद्य समस्या का प्रमुख कारण मानी जा सकती है।
(2) मांग की ऊँची आय लोच-आमतौर पर कम आय वाले लोगों
की आय का अधिकांश भाग आवश्यक वस्तुओं पर खर्च होता है परिणामस्वरूप
आय में वृद्धि होने पर अनाज की मांग तेजी से बढ़ती है। अतः कम आय वर्ग में अनाज के
लिए मांग की आय लोच बहुत अधिक रहती है।
आपूर्ति विषयक कारक
सामान्यतः
अनाज व खाद्य पदार्थों की आपूर्ति की तुलना में मांग तेजी से बढ़ती है। अल्पकालीन
हल आयात के द्वारा समय-समय पर किये जाते हैं। लेकिन दीर्घकालीन दृष्टि से आपूर्ति
सदैव कम ही रही है। इसके मुख्य कारण निम्न प्रकार से हैं :
(1) उत्पादन में धीमी और अनिश्चित वृद्धि-भारत
में भोजन का महत्वपूर्ण अंश अनाज हैं- लेकिन उपज की वृद्धि धीमी
होने के कारण आपूर्ति सदैव कम बनी रहती है। इस दिशा में हरित क्रान्ति एक कदम था
लेकिन उसका लाभ केवल कुछ क्षेत्रों तक तथा जो कुछ फसलों तक सीमित हो गया।
परिणामस्वरूप अन्य फसलों की उपज तुलनात्मक रूप में कम रही, साथ ही सूखा व बाढ़ आदि
ने भी अनाज की कमी को बढ़ाया है। परिणामस्वरूप अनाज की आपूर्ति कम व अनिश्चित बनी
रहती है। जिससे खाद्य समस्या और अधिक उलझ जाती है।
(2) कम और घटती-बढ़ती आपूर्ति-भंडारण व विपणन की अपर्याप्त
सुविधा के कारण खेतिहर अपनी उपज को कीट-पतंगों व चूहों आदि से
नहीं बचा पाते हैं इससे फसल का एक तिहाई भाग नष्ट हो जाता है और शहरी आबादी के
संदर्भ में समस्या गम्भीर रूप धारण कर लेती है। कभी-कभी लाभ कमाने की चेष्टा से
किसान भंडारण कर बाजार में आपूर्ति कम कर देते हैं। जिससे खाद्य समस्या उत्पन्न हो
जाती है।
निर्धनता
भारत
में निर्धनता एक अभिशाप है खाद्य समस्या गरीबों के संदर्भ में और बुरी होती है
इसके निम्न कारण हैं-
(1) अपर्याप्त क्रयशक्ति-सामान्यतः गरीबों के पास पर्याप्त
क्रय शक्ति नहीं होने के कारण वे अपेक्षित मात्रा में वस्तुएँ
खरीदने में असमर्थ रहते हैं और जब फसल की स्थिति खराब होती है तो यह स्थिति और
अधिक दयनीय हो जाती है।
(2) कामकाज का अभाव व बड़े परिवार-हमारे समाज का एक वर्ग ऐसा है जिसके पास कोई परिसम्पत्ति
नहीं है। परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक है और उसे काम भी नहीं मिलता है तो
समस्या और कठिन हो जाती है।
आयात
और निर्यातः सरकार द्वारा अनाज या अन्य खाद्यान्न के निर्यात के लिए लाइसेंस जारी
करती है या निर्यात की अनुमति प्रदान करती है। इसके अलावा राजनयिक आधार मानवीय
सहायता के रूप में भी गेहूँ और चावल का निर्यात करती है। 2015-16 के दौरान
केंद्रीय पूल भण्डारों से म्यांमार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगभग 100 लाख
टन चावल उपलब्ध कराया गया। खाद्य तेलों की घरेलू आपूर्ति की तुलना में मांग निरतर अधिक
बनी हुई हैं, अतः पिछले दो दशक से अधिक समय से इनका आयात करना पड़ रहा है। दालों
में भी कमोबेश यही स्थिति बनी रहती है।
बफर स्टॉक
भारत की खाद्यान्न का एक न्यूनतम भंडार बनाए रखने की एक नीति है (केवल चावल और गेहूं के लिए) जिससे कि पूरे देश में पूरे साल खरीदी जा सकने वाली कीमतों पर खाद्य पदार्थ उपलब्ध रहे। मुख्य आपूर्ति यहां से टीपीडीएस यानी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली ( 1997 में सा.वि. प्र. को ल.लि.नि.प्र. के रूप में पुनर्गठित किया गया था) को जाती है और कभी-कभी बिक्री के लिए खुले बाजार में भी ताकि कीमतें नियंत्रित हों।
पिछले कुछ वर्षों से चल रहे टीपीडीएस की वजह से खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ने और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) लागू होने के चलते सरकार ने आरक्षित भंडार मानदंड (2005) को संशोधित (2014 के मध्य में) किया।
जैसे
ही बीपीएल खंड का आय स्तर बढ़ता है (भविष्य में), खाद्यान्नों के लिए बफर परिपाटी
नीचे की दिशा में संशोधित की जाएगी। लेकिन ऐसे स्टॉक को बनाए रखने का तर्क भी काम
करता होगा सरकार द्वारा बाजार में हस्तक्षेप के उद्देश्य से।
विकेंद्रीकृत खरीद योजना
विकेंद्रीकृत
खरीद (डीसीपी) योजना को भारत सरकार ने 1997 में शुरू कर दिया था (केंद्र के साथ
कुछ राज्य सरकारें भी स्थानीय स्तर पर किसानों से अनाज खरीदती थीं)। इस योजना के
तहत निर्दिष्ट राज्य सरकार अनाज की खरीद करती थी, भंडारण करती थी और टीपीडीएस के
तहत वितरण भी करती थीं। केंद्रीय निर्गम मूल्य और राज्यों की आर्थिक लागत में अंदर
को भारत सरकार राज्यों को सब्सिडी के रूप में लौटा देती थी। खरीद की विकेंद्रीकृत
प्रणाली से एमएसपी संचालन के तहत ज्यादा-से-ज्यादा किसानों तक पहुंचा जा सकता था,
पीडीएस की कुशलता बढ़ती थी, स्थानीय स्वाद के अनुरूप अनाज की ज्यादा किस्में उपलब्ध
होती थीं और एफसीआई का ढुलाई का खर्च भी कम आता था।
भारत
सरकार ने सभी राज्यों को डीसीपी योजना अपनाने को कहा ताकि वितरण लागत कम हो सकें
और अब तक गरीब रह गए इलाकों में किसानों तक मूल्य समर्थन प्रणाली की पहुंच बढ़ाई
जा सके। दैनिक आधार पर खरीद प्रक्रिया के बारे में सूचना के प्रवाह में अंतर को
देखते हुए एक ऑनलाइन खरीद निरीक्षण तंत्र (ओपीएमएस) विकसित किया गया है ताकि देश
में गेहूं, धान और मोटे अनाज की खरीद प्रक्रिया की दैनिक आधार पर सूचना दी और
निरीक्षण किया जा सके।
भारत
सरकार के दो फैसले जो चावल और गेहूं की खरीद और भंडारण पर असर डालेंगे, वह हैं :
(i)
एमएसपी से ज्यादा और ऊपर बोनस देने की घोषणा कर रहे राज्यों की
खरीद को सीमित करना, जो टीपीडीएस और अन्य कल्याण योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) के लक्ष्य
की सीमा तक पहुंच गई है। गैर-डीसीपी के मामले में बोनस का ऐलान करने वाले राज्यों
में एफएसईआई एमएसपी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेगा।
(ii)
चावल पर कर की दर पर 25 फीसदी की रोक लगाना।
भंडारण
वर्तमान
भंडारण सुविधा न केवल क्षमता के हिसाब से बल्कि कुछ उपजों के लिहाज से भी
अपर्याप्त है। भंडारण क्षमता उत्पादन वृद्धि एवं लंबे काल तक मांग के अनुरूप
विकसित नहीं हो पाई। भंडारण की चुनौती को इस प्रकार रेखांकित किया गया है
(i)
सार्वजनिक एजेन्सियों के पास उनके द्वारा खरीदे गए गेहूं औरmचावल
की आधी मात्रा के भंडारण की भी सुविधा उपलब्ध नहीं है।
(ii)
मौसमी मुद्रास्फीति जो कि फलों-सब्जियों में आम है, को नियंत्रित रखने की प्रभावी रणनीति नहीं है।
(iii)
सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों के शीत भंडारण (Cold Storage) क्षमता
केवल 29 एमटी (योजना आयोग, 2012) है। जबकि केवल आलू का उत्पादन 35 एमटी है।
(iv)
केवल 10 प्रतिशत फलों-सब्जियों के शीत भंडारण की सुविधा है (योजना आयोग 2011)।
वैज्ञानिक
भंडारण क्षमता की आवश्यकता एवं उपलब्ध के बीच के अंतर को पाटना समय की मांग है।
इसके लिए ऐसी नीतियों को बढ़ाने की जरूरत है जिससे इस क्षेत्र में निजी के निवेश
को आकर्षित किया जा सके।
सरकारी
नीतिः विकसित देशों की तरह खेतों से सीधे उपभोक्ता तक इनकी पहुँच सुनिश्चित करने
के लिए सरकार ने कोल्ड चेन और अत्याधुनिक वेयर हाउस निर्माण की नीति को प्रस्तावित
किया है। अन्य उपायों में गोदामों के निर्माण में PPP मॉडल का भी उपयोग किया जा
रहा है।
खुला बाजार बिक्री योजना
एफसीआई
समय-समय पर खुले बाजार में गेहूं की बिक्री पूर्व निर्धारित मूल्य (आरक्षित मूल्य)
पर करता रहता है, जिसे खुले बाजार की बिक्री योजना (ओएमएसएस) कहा जाता है। इसके
लक्ष्य निम्न हैं :
(i)
अनाज की बाजार आपूर्ति बढ़ाना;
(ii)
खुले बाजार की कीमतों पर अधिकता के प्रभाव का इस्तेमाल करना, और
(iii)
अतिरिक्त भंडार को खाली करना।
खुले
बाजार में बिक्री की योजना (घरेलू) के तहत सरकार अब अलग अलग कीमत वाली नीति को
अपनाती है ताकि पुराने भंडार की बिक्री को प्रोत्साहित किया जा सके। इस नीति के
उद्देश्य हैं :
(i)
आरक्षित मूल्य को एमएसपी से ऊपर रखना लेकिन कमाई के मूल्य या
गेहूं के आर्थिक मूल्य से यथोचित कम रखना ताकि कटाई के मौसम में खरीदारों का
मंडियों से गेहूं खरीदने के प्रति आकर्षण बना रहे और बाजार प्रतिस्पर्धी बना रहे।
(ii)
यह स्थिति बनाए रखना कि कमी के मौसम में भी बाजार मूल्य ज्यादा न
बढ़ें और मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहे।
पिछले दशकों में खाद्य नीति की विफलताएँ
सरकार
की खाद्य नीति की विफलता का संबंध अकुशल प्रबंधन से जुड़ा हुआ है क्योंकि देश में
अनाज के संबंध में भारी क्षेत्रीय असमानताएं विद्यमान हैं जो कि गंभीर समस्या है।
अनाज का उत्पादन बढ़ा तो हैं लेकिन संतोषजनक नहीं है। इस संदर्भ में एक बात का
स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि हमारी खेती अभी भी मौसम की दासता से है तथा दालों
की उपज में वृद्धि की दर बहुत कम है।
अनाज
वसूली की नीति की विफलता और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अनाज सुलभ कराने के
लिए आयात पर निर्भरता के परिणामस्वरूप अनाज की उपज बढ़ाने के प्रयत्नों पर
प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिससे कीमतों में वृद्धि हुई है।
खाद्य
समस्या के स्वरूप, प्रस्तावित समाधानों और सरकारी नीति के उपयुक्त विवेचन से यह
स्पष्ट होता है कि यह समस्या बड़ी भी है और मुक्त नहीं गम्भीर भी है। सरकारी नीति
अभी भी इस चुनौती का सामना करने में पर्याप्त सफलता प्राप्त नहीं कर पाई है अत: एक
उचित खाद्य नीति क्या हो यह एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है।
भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक उचित खाद्य नीति
भारत
में जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ खाद्यान्नों की मांग में तेजी से वृद्धि हो रही
है। योजनाओं में सार्वजनिक व निजी विनियोग के बढ़ने से खाद्यान्नों के लिए
'प्रभावपूर्ण माँग' का बढ़ना स्वाभाविक है। सरकार ने खाद्य समस्या को हल करने के
कई प्रयत्न किए हैं, लेकिन उसको खाद्य-समस्या के सभी पहलुओं के उचित हल निकालने
में अभी तक पूरी सफलता नहीं मिली है। खाद्य-समस्या को हल करने के लिए निम्नलिखित सुझाव
दिये जा सकते हैं :
(1) आधुनिक व गहन खेती की आवश्यकता
भारत
में नई भूमि पर विस्तृत खेती की सम्भावनाएँ बहुत कम हैं। अत: वर्तमान कृषित भूमि
पर गहन खेती के उपाय अपनाकर प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि की जानी चाहिए। इसके लिए
सुधरे हुए बीजों, उत्तम खाद और रासायनिक उर्वरकों, उत्तम हल तथा अन्य औजारों और
खेती के सुधरे हुए तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। सिंचाई के विस्तार द्वारा जिन
खेतों पर एक फसल उगाई जाती है उन पर दो या अधिक फसलें उगाई जानी चाहिए।
(2) वर्षा पर आश्रित तथा सूखी खेती के विस्तार की आवश्यकता
वर्षा
पर आश्रित क्षेत्रों में सूखी खेती की विधियों को अपनाकर अनाज का उत्पादन बढ़ाया
जा सकता है। इन क्षेत्रों में उपलब्ध नमी की रक्षा करने की आवश्यकता है। पानी को
तालाबों व बन्धों आदि में संग्रह करके रखना चाहिए ताकि वह पूरक सिंचाई के रूप में
इस्तेमाल किया जा सके। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखी विधियों को अपनाकर
खरीफ की फसलों को सूखे के प्रभाव से बचाया जा सकता है। रबी की फसलों के लिए बोने
से पूर्व सिंचाई की जा सकती है।
बागवानी,
चारे व फार्म वानिकी के कार्यक्रम अपनाये जाते हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय
वाटरशेड विकास कार्यक्रम लागू किया है। वाटरशेड वह भू-क्षेत्र होता है जिसे पीछे
से पानी की सप्लाई नहीं मिलती, बल्कि जिस पर बरसने वाला जल भी शीघ्र बहकर आगे निकल
जाता है। इसलिए उसके जल संरक्षण व सदुपयोग के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। सूखी खेती
में उचित मात्रा में उर्वरकों व औजारों का उपयोग करके शीघ्र पक कर तैयार होने वाली
फसलों का प्रयोग बढ़ाया जाता है। अतः स्पष्ट है कि भारत में बहुचर्चित दूसरी हरित
क्रांति सूखी-कृषि की ही क्रान्ति होगी।
(3) प्रति व्यक्ति अनाज व दालों के उपभोग में स्थिरता या गिरावट की समस्या को हल किया जाना चाहिए
योजना
आयोग के पूर्व सदस्य डॉ. सी.एच. हनुमन्था राव का मत है कि देश में प्रति व्यक्ति
खाद्यान्नों के उपभोग में गिरावट का प्रमुख कारण यह है कि विकसित प्रदेशों में
ग्रामीण क्षेत्रों में आमदनी बढ़ी है, जहाँ खाद्यान्नों की माँग-आय-लोच (Income
elasticity of demand of foodgrains) बहुत नीची है। इससे इन क्षेत्रों में
खाद्यान्नों का प्रति व्यक्ति उपभोग बढ़ने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि लोगों
का खाद्यान्नों के उपभोग का स्तर पहले ही काफी ऊँचा है। देश के अन्य भागों में
निर्धन लोगों के पास क्रय-शक्ति का अभाव रहता है, जिससे वे पर्याप्त मात्रा में
अनाज नहीं खरीद पाते। इस प्रकार दोनों तरह के प्रदेशों या क्षेत्रों में
खाद्यान्नों के प्रति व्यक्ति उपभोग में गिरावट अथवा नीचा रहने की हो दशाएँ पाई
जाती हैं।
(4) फसलों की रक्षा
भारत
में प्रति फसल का एक बड़ा हिस्सा टिड्डियों, चूहों, कीड़ों, फसलों के रोगों से
नष्ट हो जाता है। कीड़े मारने की दवाओं के प्रयोग से भी फसलों को रोग नहीं लगता।
फसलों को बाढ़, अनावृष्टि व अन्य खतरों से बचाने के लिए इनका बीमा कराया जाना
चाहिए। उपज को साल भर सुरक्षित रखने के अभाव में बड़ी मात्रा में अनाज नष्ट हो
जाता है। खेती की पैदावार को उचित संग्रह के लिए गोदामों और भण्डारगृहों का
विस्तार किया जाना चाहिए।
(5) संस्थागत परिवर्तन
इनके
अन्तर्गत भूमि-सुधार व बिक्री सम्बन्धी नए संगठनों आदि का समावेश किया जाता है।
पिछले वर्षों में इस बात पर पुनः जोर दिया गया है कि भूमि सुधारों को
शीघ्रतापूर्वक लागू करके ही कृषि का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में एक
महत्वपूर्ण प्रश्न जोतों को बड़ा करने का है। बहुत छोटी जोतों पर गहरी खेती के
उपायों को अपनाकर भी उत्पादन बढ़ाने में विशेष सफलता नहीं मिल सकती।
(6) विस्तार कार्यों के लिए प्रभावशाली संगठन
केवल
संस्थागत परिवर्तन से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें एक ऐसा संगठन बनाना होगा जो
कृषकों तक आवश्यक कृषिगत साधन तेजी से एवं उचित समय पर पहुंचा सके और उन्हें
उत्पादन बढ़ाने में उचित मदद व प्रेरणा दे सके। सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं जैसे
ग्राम पंचायतों, सहकारी संगठनों, जिला ग्रामीण-विकास-एजेंसियों (CRDA) आदि को अधिक
सक्रिय व सफल बनाया जाना चाहिए। कृषकों को कृषिगत साधन-खाद, बीज, कीटनाशक दवाएँ
आदि उचित समय पर उचित मूल्यों पर उचित मात्रा में उपलब्ध की जानी चाहिए। इस
सम्बन्ध में प्रशासनिक कार्य कुशलता बढ़ानी चाहिए।
(7) देशव्यापी सार्वजनिक वितरण की प्रणाली का महत्व
अनाज
के वितरण की एक ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे देश के सभी भागों, विशेषकर
ग्रामीण क्षेत्रों में आम नागरिकों को साल भर उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में
अनाज उपलब्ध हो सके। प्रायः देखा जाता है कि जब किसी स्थान पर किसी समय फसल बिगड़
जाती है या अन्य कारणों से अनाज की पूर्ति घट जाती है या माँग बढ़ जाती है तो
किसान व व्यापारी तथा कुछ सीमा तक उपभोक्ता भी आवश्यकता से अधिक मात्रा में अनाज
का संग्रह करने लगते हैं जिससे अनाज के भाव ऊँचे हो जाते हैं। इस समस्या को हल
करने के लिए अशोक मेहता समिति ने मूल्यों के स्थिरीकरण का सुझाव दिया था।
(8) उपभोग में सुधार
एक
औसत भारतवासी के दैनिक भोजन में अनाज की प्रधानता होती है। अनाज के स्थान पर केले,
शकरकन्द, व आलू आदि अधिक उपज देने वाली फसलों पर उपभोग बढ़ाया जाना चाहिए तथा फल,
सब्जी, अंडे, मांस-मछली आदि पौष्टिक पदार्थों का उत्पादन बढ़ाकर तथा इनकी कीमतें नीची
रखकर सर्वसाधारण द्वारा इनके उपभोग में वृद्धि की जानी चाहिए, ताकि कम अनाज से काम
चलाया जा सके और आम नागरिक की दैनिक खुराक की गुणवत्ता में भी सुधार किया जा सके।
(9) जनसंख्या का नियन्त्रण
खाद्यान्नों
की समस्या का स्थायी हल करने के लिए कृषिगत उपज बढ़ाने, फसलों की रक्षा तथा उपभोग
में सुधार करने के साथ-साथ राष्ट्रीय परिवार योजना आन्दोलन द्वारा जनसंख्या वृद्धि
की रफ्तार को भी कम किया जाना चाहिए। जनसंख्या की वृद्धि पर नियंत्रण स्थापित किए
बिना खाद्यान्नों में स्थायी आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में कठिनाई होगी। भारत में
जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि को 1.8 प्रतिशत से नीचे लाने का प्रयास तेज किया जाना
चाहिए।
सरकार की नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम
समन्वित बाल विकास सेवा योजना
यह
योजना 1975 में चालू की गई और इसका उद्देश्य बच्चों एवं गर्भवती स्त्रियों एवं दूध
पिलाने वाली माताओं को खाद्य-सहायता उपलब्ध कराना था। "पिछले दो दशकों के
अनुभव से पता चलता है कि सबसे जरूरतमंदों को कई बार यह सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती
और जब हो भी पाती है तो यह अधिकार के लिए अनुपूरक की अपेक्षा प्रतिस्थापक का कार्य
करती है। "1996 के समन्वित बाल विकास सेवा प्रोग्राम में देश के 4,200 ब्लाकों
और इनके साथ 5.92 लाख आंगनबाड़ियों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। इसके
परिणामस्वरूप, लाभ-प्राप्तकर्ताओं तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। इसके
परिणामस्वरूप, लाभ-प्राप्तकर्ताओं की संख्या 185 लाख बच्चों और 37 लाख माताओं तक
पहुंच गई। इस प्रोग्राम की समीक्षा से यह पता चला कि जहां इस प्रोग्राम के अधीन
क्षेत्रों में स्तनपान कराने वाली 25 प्रतिशत माताओं ने अपने
बच्चों को छ: मास तक खाद्य अनुपूरकों (Food supplement) से लाभ पहुंचाया, इससे गैर-आई.सी.डी.एस.
क्षेत्रों में केवल 19 प्रतिशत को लाभ प्राप्त हुआ।'' ये
मूल्यांकन इस कठोर सत्य की ओर संकेत करता है कि आई.सी.डी.एस. प्रोग्राम से प्राप्त
लाभ प्रभावी रूप में पोषण-स्तर को उन्नत नहीं कर पाए।
दोपहर के भोजन (मीड-डे-मील) का प्रोग्राम
दोपहर
के भोजन का प्रोग्राम 2-14 वर्ष की आयु के बीच आंगनवाड़ी, स्कूलों में जाने वाले
बच्चों के लिए आरम्भ किया गया था। इस प्नोग्नाम को अब नया नाम दिया गया है
प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता और इसे 1975 के बाद प्राथमिक शिक्षा स्तर पर
4,480 ब्लॉकों में सर्वव्यापक रूप में लागू किया जा रहा है। मार्च, 1997 तक लगभग 6
करोड़ स्कूलों में बच्चे इस प्रोग्राम के आधीन लाए गए। दोपहर के भोजन का प्रोग्राम
तमिलनाडु, कर्नाटक और दक्षिण के अन्य राज्यों में सफल हुआ है, यह उत्तर भारत के
राज्यों में विफल हुआ है। अनाजों का उत्पादन जनसंख्या की वृद्धि दर की तुलना में
अधिक तेजी से बढ़ा है, परन्तु दालों का उत्पादन जनसंख्या की वृद्धि दर की तुलना
में पिछड़ गया है। परिणामतः दालों का प्रति व्यक्ति उपभोग 60.7 ग्राम से कम होकर
42 ग्राम हो गया।
इसके
अतिरिक्त, चिन्ता का एक और क्षेत्र उद्यान खेती (Horticulture) की ओर अपर्याप्त
ध्यान देना है और इसके नतीजे के रूप में सब्जियों की उपलब्धि, विशेषकर हरे पत्ते
वाली सब्जियों और पीली अथवा लाल सब्जियों की पूरे साल के दौरान उपलब्धि प्रभावित
हुई है और शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की सामर्थ्य के अनुसार सब्जियाँ
मुहैया कराना एक स्वप्न हो रहा है। आय के स्तर का दालों, दूध, फलों, मांस, तेल और चीनी
के उपभोग के साथ सकारात्मक सम्बन्ध है।
दालों
के संबंध में 40 ग्राम प्रतिदिन की सिफारिश की गई है।
1996-97 में राष्ट्रीय औसत 34 ग्राम पर आ जाने से गरीबों की दालों के उपभोग के बारे में स्थिति बदतर हो गई थी। क्षेत्रानुसार केवल कर्नाटक, मध्य
प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में दालों का औसत उपभोग राष्ट्रीय स्तर पर
सिफारिश किए गए 40 ग्राम प्रतिदिन से ऊंचा है। जब तक दालों का उत्पादन महत्वपूर्ण
रूप में नहीं बढ़ाया जाता, पोषण के स्तरों में और गिरावट आएगी।
यदि
परिवार के सभी सदस्यों को पोषण-शिक्षा (Nutrition education) दी जाए. तो इससे
परिवार के आन्तरिक वितरण में काफी सुधार हो सकता है। इससे उपलब्ध साधनों को हरी और
पत्तेदार सब्जियों की ओर मोड़ने की ओर सहायता मिल सकती है और इससे आयोडीन-युक्त
नमक के प्रयोग से आयोडीन के अभाव को कम करने में भी सहायता प्राप्त हो सकती है।
पोषण-शिक्षा
परिवार के सभी सदस्यों को देने से यह बात सुनिश्चित की जा सकती है कि गर्भवती और
दूध पिलाने वाली स्त्रियों को अपने सामान्य भोजन से 16 से 20 प्रतिशत अधिक खिलाया
जाए। इससे कम वजन वाले बच्चों के जन्म को कम किया जा सकता है और उन्हें अपने जीवन
को अच्छे रूप से आरम्भ करने में सहायता मिल सकती है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली
सार्वजनिक
वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य 1960-70 के दशक में खाद्य-दुर्लभता के समय
उपभोक्ता के लिए एक कीमत आलम्बन कार्यक्रम (Price Support
Programme) का काम करना था। अत: इस प्रकार यह कीमत-स्थिरीकरण
(Price stabilisation) के उपकरण रूप में कार्य करने लगी और निजी व्यापारियों के
विरुद्ध एक प्रतिशक्ति के रूप में उभरी क्योंकि व्यापारी दुर्लभता की स्थिति का
फायदा उठाते हुए अपने लाभ को अधिकाधिक करने का प्रयास करते थे। इसका मूल उद्देश्य
अनिवार्य वस्तुओं अर्थात् चावल, गेहूं, चीनी, खाद्य तेल, सॉफ्ट कोक और मिट्टी का
तेल साहय्यित दरों (Subsidized Rates) पर उपलब्ध कराना था।
देश
में आज 4.62 लाख से अधिक उचित मूल्य की दुकानों का नेटवर्क बन गया है जो 30,000
करोड़ रुपये की वस्तुएं प्रति वर्ष वितरित करती हैं। अतः भारतीय सार्वजनिक वितरण
प्रणाली संभवतः विश्व में सबसे बड़ा वितरण नेटवर्क (Distribution network) है। कई
रोजगार जनन कार्यक्रमों (Employment Generation Programmes) में मजदूरी के अंग के
रूप में सहाय्यित खाद्यान्न वितरित किए गए।
चाहे
चावल, गेहूं, चीनी, खाद्य तेल, साफ्ट कोक और मिट्टी का तेल सार्वजनिक वितरण
प्रणाली की दुकानों पर बेचे जाते हैं किन्तु इनमें से चार मदों अर्थात् चावल,
गेहूं, चीनी और मिट्टी का तेल कुल विक्रय में भाग 86 प्रतिशत है। केवल चीनी का भाग
35 प्रतिशत, चावल का 27 प्रतिशत, गेहूँ का 10 प्रतिशत और मिट्टी
के तेल का प्रतिशत है। मोटे अनाज (बाजरा, ज्वार और अन्य अनाज)
जिनका उपयोग गरीब वर्गो द्वारा किया जाता है का कुल विक्रय में भाग 1 प्रतिशत से
भी कम है। दालें जो गरीबों के लिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत है का भाग 0.2 प्रतिशत से
भी कम है।
जब
तक विकास प्रक्रिया बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में गरीबी कम करने
में सफल नहीं होती, तब तक इन गरीब राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जारी
रखना न्यायोचित होगा। बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि इस योजना को उचित रूप में
लक्षित बनाया जाए ताकि इससे बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकें और गरीब राज्यों में
इस योजना को पूरी तरह लागू करने की इच्छाशक्ति मजबूत बनाई जा सके।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार की नीति
सार्वजनिक
वितरण प्रणाली का सर्वोच्च लक्ष्य गरीबों की मदद करना है। इसके लिए गरीबों की
पहचान बुनियादी समस्या है और इसके लिए ऐसी रणनीति तैयार की जानी चाहिए जो
अर्थव्यवस्था सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभों को गैर- निर्धनों तक पहुंचने की
क्रिया को सरल बना सके। इसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के लक्ष्य की
प्राप्ति के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं :
1.
गरीबों की पहचान के कार्य को नौकरशाही की अपेक्षा पंचायती राज
संस्थाओं को सौंप देना चाहिए। इस प्रश्न पर अर्थशास्त्रियों और समाज सेवकों में
एकमत प्राप्त हो चुका
2.
विस्तृत उपभोक्ता सर्वेक्षणों द्वारा ऐसी वस्तुओं की पहचान की जानी चाहिए जो सार्वजनिक वितरण में गरीबों को अधिक आय-हस्तांतरण में सहायक
हो सके और अन्य वस्तुएं जो गैर-निर्धनों द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं। धीरे-धीरे
खुले बाजार में हस्तांतरित कर देनी चाहिए।
3.
गरीबों को प्रभावी रूप से आय-हस्तांतरण के लिए अनिवार्य वस्तुओं की
जारी कीमत (Issue Price) और बाजार कीमत में काफी अन्तर चाहिए ताकि सार्वजनिक वितरण
प्रणाल वस्तुओं को खरीदने के लिए गरीब आकर्षित हो सकें।
4.
सार्वजनिक वितरण प्रणाली को रोजगार जनन कार्यक्रमों जैसे जवाहर
रोजगार योजना या रोजगार आश्वासन योजना के माध्यम से लागू करना चाहिए क्योंकि इन
प्रोग्रामों के गरीबों को दोहरे लाभ प्राप्त होते हैं। प्रथम, इनमें गैर निर्धनों
के समावेश की त्रुटि न्यूनतम हो जाती है क्योंकि ऐसा प्रायः देखा गया है कि गैर- निर्धन
सामान्यत: इन रोजगार कार्यक्रमों का लाभ नहीं उठाते। द्वितीय, निर्धनता समाप्ति
रोजगार जनन कार्यक्रमों में क्रय-शक्ति गरीबों को हस्तांतरित करने के अतिरिक्त
सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा अतिरिक्त आय भी इन वस्तुओं के माध्यम से
लाभप्राप्तकर्ताओं को उपलब्ध कराई जाएगी।
5.
पंचायती राज संस्थाओं को अपने लक्षित उद्देश्यों से विकृत होने से रोकने के लिए यह अच्छा होगा कि ऐसी गैर-सरकारी संस्थाओं को जिनका
गरीबों की सहायता करने में रिकार्ड सिद्ध हो चुका हो, पंचायती राज संस्थाओं के
निरीक्षण के साथ जोड़ा जाए।
6.
राज्य सरकार को खाद्य-स्टाम्प (Food Stamps) या प्रमाण पत्र (Vouchers) पंचायती राज
संस्थाओं को जारी कर देने चाहिए ताकि वे इनको जवाहर रोजगार
प्रोग्राम या रोजगार आश्वासन प्रोग्राम के चालकों को श्रमिकों में बांटने के लिए
सौंप दें।
7.
भारतीय खाद्य निगम गरीबों को खाद्य-सुरक्षा उपलब्ध कराने का सबसे
उचित संस्थान नहीं है। यह कहीं बेहतर होगा यदि भारतीय खाद्य निगम को खाद्य-कीमतों
को स्थिर करने की जिम्मेदारी दी जाए और पंचायती राज संस्थाओं को खाद्यान्न के
आवंटन का कार्य राज्य सरकारों को सौंप दिया जाए।
गरीबों
की पहचान के लिए ग्रामीण क्षेत्रों निम्नलिखित कसौटियों का प्रयोग सहायक सिद्ध हो
सकता है :
(क)
सभी परिवार जो रोजगार कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, शामिल किए जाने
चाहिएँ।
ख)
बच्चों के साथ अकेली माताएं या बिना आलम्बन के विधवाएं इसमें शामिल की जानी चाहिए।
(ग)
सभी भूमिहीन कृषि श्रमिक, छोटे दस्तकार इसमें शामिल किए जाने चाहिएं।
शहरी क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित कसौटियाँ अपनानी चाहिए :
(i)
क्षेत्रों का ध्यानपूर्वक चुनाव : गन्दी बस्तियाँ ऐसे क्षेत्र जो परम्परा से गरीब सम्प्रदायों के निवास हैं जैसे कुम्हार, मोची, निर्माण श्रमिक, गरीब
गृह आधारित श्रमिक आदि।
(ii)
सभी आय-कर न अदा करने वाले परिवार शामिल करने चाहिए।
(iii)
ऐसे परिवार जिनके पास महंगी चिरस्थायी उपभोक्ता वस्तुएं न हो जैसे
रसोई-गैस, रेफ्रिजिरेटर, वाशिंग मशीन, टेलीफोन आदि।
निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यक्षेत्र विस्तृत है और इस कारण यह गरीब वर्ग के बड़े भाग को सहायता पहुंचा सकती है, यदि इसे उचित रूप में लक्षित किया जाए। फिर भी वस्तु-स्थिति यह है कि इसका गरीबों को लाभ रक्त संचारण (Blood transfusion) की भांति है जिससे अस्थायी राहत प्राप्त हो सकता है। गरीबों को स्थायी खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए ऐसी रणनीतियों पर बल देना उचित होगा जो गरीबों को कम करें। इस संबंध में तीव्र आर्थिक विकास के साथ अधिक रोजगार जनन का महत्व केन्द्रीय स्थान रखता है। इस बात को आश्वस्त करने के लिए कि गरीबों को आय के रूप में प्राप्त लाभ कीमतों में वृद्धि के परिणामस्वरूप लोप न हो जाएं, यह जरूरी है कि सरकार कीमत-स्थिरीकरण (Price stabilisation) रणनीतियों को अपनाएं।