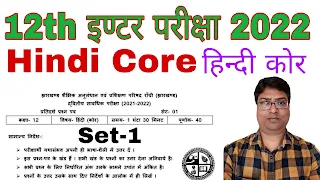01. निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गये प्रश्नों के उत्तर लिखिए-
02+02+02= 06
चारूचंद्र की चंचल किरणें,
खेल रही हैं जल-थल में,
स्वच्छ चाँदनी बिछी हुई है,
अवनि और अम्बर तल में।
पुलक प्रकट करती है धरती,
हरित तृणों की नोंकों से,
मानो झूम रहे हैं तरू भी,
मंद पवन के झोंकों से।
(क) धरती और आकाश का कैसा सौन्दर्य दिखता है?
उत्तर:
धरती और आकाश में निर्मल चाँदनी अपनी छटा बिखेतरी है, जिसके कमल चारों तरफ मनोहारिणी
शोभा दिखाई देती है।
(ख) चन्द्रमा की चंचल किरणें कहाँ क्रीड़ा कर रही हैं?
उत्तर:
जल और थल में क्रीड़ा कर रही है।
(ग) कविता की प्रथम पंक्ति में कौन-सा अलंकार है?
उत्तर:
उपमा अलंकार।
अथवा
निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गये प्रश्नों के उत्तर लिखिए-
हम अपने जीवन में सुख-समृद्धि चाहते हैं, ज्ञान, शांति और कीर्ति चाहते
हैं, किंतु ये चीजें हमें तभी मिल पाती हैं जब हम इनको पाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील
बने रहो हम अपने समय के एक एक क्षण- को बहुमूल्य मानकर उसका सदुपयोग करें तथा निरंतर
परिश्रम करते रहें। यह तभी संभव होगा, जब हम अपने समय का सही विभाजन और नियोजन कर लें,
क्योंकि समय सीमित है और करने के लिए काम अनंत हैं। जो काम आवश्यकता और महत्व की दृष्टि
से पहले पूरे करने हैं, उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए। ध्यान रहे कि सभी कामों को सफलतापूर्वक
पूरा करने के लिए अच्छा स्वास्थ्य और प्रबल इच्छाशक्ति होनी चाहिए।
(क) जीवन में सुख-समृद्धि कैसे प्राप्त की जा सकती है?
उत्तर:
जीवन में सुख-समृद्धि निरंतर परिश्रमशील तथा सुनियोजित होने से पाई जा सकती है।
(ख) समय का विभाजन और नियोजन करना क्यों आवश्यक है?
उत्तर:
ढेर सारे कार्यों को सफलता और सुविधापूर्वक करने के लिए समय का विभाजन और नियोजन आवश्यक
है।
(ग) इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए?
उत्तर:
सुख-समृद्धि के सूत्र ।
खंड
- 'ख'
(अभिव्यक्ति
और माध्यम तथा रचनात्मक लेखन)
02. निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए 05+05=10
(क) 'समाचार पत्र' अथवा 'प्रदूषण' पर एक निबंध लिखिए।
उत्तर:
(क) 'समाचार पत्र'
भूमिका-समाचार-पत्र
वह कड़ी है जो हमें शेष दुनिया से जोड़ती है। जब हम समाचार-पत्र में देश-विदेश की खबरें
पढ़ते हैं तो हम पूरे विश्व के अंग बन जाते हैं। इससे हमारे हृदय का विस्तार होता है।
लोकतंत्र
का प्रहरी-समाचार-पत्र लोकतंत्र का सच्चा पहरेदार है। उसी के माध्यम से लोग अपनी इच्छा,
विरोध और आलोचना प्रकट करते हैं। यही कारण है कि राजनीतिज्ञ समाचार-पत्रों से बहुत
डरते हैं । नेपोलियन ने कहा था-"मैं लाखों विरोधियों की अपेक्षा इन समाचार-पत्रों
से अधिक भयभीत रहता हूँ समाचार-पत्र जनमत तैयार करते हैं। उनमें युग का बहाव बदलने
की ताकत होती है। राजनेताओं को अपने अच्छे-बुरे कार्यों का पता इन्हीं से चलता है।
प्रचार
का उत्तम माध्यम-आज प्रचार का युग है। यदि आप अपने माल को, अपने विचार को, अपने कार्यक्रम
को या अपनी रचना को देशव्यापी बनाना चाहते हैं तो समाचार-पत्र का सहारा लें। उससे आपकी
बात शीघ्र सारे देश में फैल जाएगी। समाचार-पत्र के माध्यम से रातों-रात लोग नेता बन
जाते हैं या चर्चित व्यक्ति बन जाते हैं। यदि किसी घटना को अखबार की मोटी सुर्खियों
में स्थान मिल जाए तो वह घटना सारे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। देश के लिए
न जाने कितने नवयुवकों ने बलिदान दिया, परन्तु जिस घटना को पत्रों में स्थान मिला,
वे घटनाएँ अमर हो गई।
व्यापार
में लाभ-समाचार-पत्र व्यापार को बढ़ाने में परम सहायक सिद्ध हुए हैं। विज्ञापन की सहायता
से व्यापारियों का माल देश में ही नहीं विदेशों में भी बिकने लगता है। रोजगार पाने
के लिए भी अखबार उत्तम साधन है। हर बेरोजगार का सहारा अखबार में निकले नौकरी के विज्ञापन
होते हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी या गैर-सरकारी फर्मे अपने लिए कर्मचारी ढूँढ़ने के
लिए अखबारों का सहारा लेती है। व्यापारी नित्य के भाव देखने के लिए तथा शेयरों का मूल्य
जानने के लिए अखबार का मुँह जोहते हैं।
जे,
पार्टन का कहना है-'समाचार-पत्र जनता के लिए विश्वविद्यालय हैं।' उनमें हमें केवल देश-विदेश
की गतिविधियों की जानकारी ही नहीं मिलती, अपितु महान विचारकों के विचार पढ़ने को मिलते
हैं। उनसे विभिन्न त्योहारों में महापरुषों के महत्त्व का पता चलता है। महिलाओं को
घर-गहस्थी सम्हालने के नए-नए नुस्खों का पता चलता हैं । प्रायः अखबार में ऐसे कई स्थायी
स्तम्भ होते हैं जो हमें विभिन्न जानकारियाँ देते हैं।
आजकल
अखबार मनोरंजन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ चले हैं। उनमें नई-नई कहानियाँ, किस्से, कविताएँ
तथा अन्य बालोपयोगी साहित्य छपता हैं। दरअसल, आजकल समाचार-पत्र बहुमुखी हो गया है ।
उसके द्वारा चलचित्र, खेलकूद, दूरदर्शन, भविष्य-कथन, मौसम आदि की अनेक जानकारियाँ मिलती
हैं।
समाचार-पत्र
के माध्यम से आप मनचाहे वर-वधू ढूँढ सकते हैं मकान, गाड़ी, वाहन खरीद-बेच सकते हैं
। खोए गए बन्धु को बुला सकते हैं। अपना परीक्षा-परिणाम जान सकते हैं। इस प्रकार समाचार-पत्रों
का महत्त्व बहुत अधिक हो गया है।
'प्रदूषण'
प्रदूषण
का अर्थ-प्रदूषण का अर्थ है-प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना । न शुद्ध वायु मिलना,
न शुद्ध जल मिलना, न शुद्ध खाद्य सामग्री मिलना, न शांत वातावरण मिलना । प्रदूषण कई
प्रकार का होता है । प्रमुख प्रदूषण हैं-वायु-प्रदूषण, जल-प्रदूषण और ध्वनि-प्रदूषण
।
वायु-प्रदूषण-महानगरों
में यह प्रदूषण अधिक फैला हुआ है। वहाँ चौबीसों घंटे कल-कारखानों का धुआँ, मोटर-वाहनों
का काला धुआँ इस तरह फैल गया है कि स्वस्थ वायु में साँस लेना दुर्लभ हो गया है। यह
समस्या वहाँ अधिक होती है जहाँ सघन आबादी होती है और वृक्षों का अभाव होता है।
जल-प्रदूषण-कल-कारखानों
का दूषित जल नदी-नालों में मिलकर भयंकर जल-प्रदूषण पैदा करता है । बाढ़ के समय कारखानों
का दषित जल नदी-नालों में घुल-मिल जाता है । इससे अनेक बीमारियाँ पैदा होती हैं।
ध्वनि-प्रदूषण-मनुष्य
को रहने के लिए शांत वातावरण चाहिए। परन्तु आजकल कल-कारखानों का शोर, यातायात का शोर,
मोटर-गाड़ियों की चिल्ल-पों, लाउडस्पीकरों की कर्णभेदक ध्वनि ने बहरेपन और तनाव को
जन्म दिया है।
प्रदूषणों
के दुष्परिणाम-उपर्युक्त प्रदूषणों के कारण मानव के स्वस्थ जीवन को खतरा पैदा हो गया
है । खुली हवा में लंबी साँस लेने तक को तरस गया है आदमी । गंदे जल के कारण कई बीमारियाँ
फसलों में चली जाती हैं. जो मनुष्य के शरीर में पहुंचकर घातक बीमारियाँ पैदा करती हैं
। पर्यावरण प्रदूषण के कारण न समय पर वर्षा आती है, न सर्दी-गर्मी का चक्र ठीक चलता
है। सूखा, बाढ़, ओला आदि प्राकृतिक प्रकोपों का कारण भी प्रदूषण है।
प्रदूषण
के कारण-प्रदूषण को बढ़ाने में कल-कारखाने, वैज्ञानिक साधनों का अधिकाधिक उपयोग, फ्रिज,
कूलर, वातानुकूलन, ऊर्जा संयंत्र आदि दोषी हैं । वृक्षों को अंधाधुंध काटने से मौसम
का चक्र बिगड़ा है । घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हरियाली न होने से भी प्रदूषण बढ़ा
है।
प्रदूषण
का निवारण-विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से बचने के लिए चाहिए कि अधिकाधिक वृक्ष लगाए
जाएँ, हरियाली की मात्रा अधिक हो । सड़कों के किनारे घने वृक्ष हों। आबादी वाले क्षेत्र
खुले हों, हवादार हों, हरियाली से ओतप्रोत हों। कल-कारखानों को आबादी से दूर रखना चाहिए
और उनसे निकले प्रदूषित मल को नष्ट करने के उपाय किये जाने चाहिए ।
(ख) अपने क्षेत्र में मच्छरों के बढ़ते प्रकोप का वर्णन करते हुए किसी
दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए।
उत्तर: सेवा में,
सम्पादक महोदय, हिन्दुस्तान, ध्रुवा, राँची
महोदय,
हमारे क्षेत्र आजाद नगर में मच्छरों का
प्रकोप निरन्तर बढ़ता जा रहा है। बस्सात तो बरसात ही है, अन्य मौसमों में भी इस घनी
आबादी वाले क्षेत्र की नालियाँ गंदे जल से भरी रहती हैं। जमा हुआ पानी तो मच्छरों की
संख्या में तीव्र गति से वृद्धि करता है। हमारे घरों में शाम होते ही सैकड़ों की संख्या
मच्छर प्रकट हो जाते हैं तथा हमारा रक्तपान करके वे अपनास्वास्थ्य सुधारने में व्यस्त
हो जाते हैं। इन मच्छरों पर तो 'कछुआ छाप अगरबत्ती' का प्रभाव होता है नहीं ये 'नाइट
क्वीन' से भयभीत होते हैं। हमारे क्षेत्र में अनेक लोग मलेरिया से ग्रस्त हैं। अब डेंगू
भी अपनी लीला दिखाने को तत्पर है।
सम्बद्ध अधिकारी शीघ्र ही इस समस्या का समाधान
करें। इस क्षेत्र की सफाई के साथ-ही-साथ मलेरिया निरोधक दवाइयों के छिड़काव की अविलम्ब
व्यवस्था करायी जाय अन्यथा इस क्षेत्र में मलेरिया एवं डेंगू के कारण अनेक लोगों की
जान से हाथ धोना पड़ सकता है।
भवदीय
दिनांक : 28 मार्च 2022. दीपक कुमार, +2 उ०वि० गोपीकांदर
(ग) अपने क्षेत्र में नियमित साफ-सफाई के लिए संबंधित पदाधिकारी को
पत्र लिखिए।
उत्तर:
सेवा में,
स्वास्थ्य अधिकरी
राँची नगर निगम, राँची।
विषय-शहर
में स्वच्छता एवं सफाई हेतु प्रपत्र ।
श्रीमान्
हम आपका ध्यान राँची शहर के अशोक नगर महोल्ले
की सफाई संबंधी दुर्व्यवस्था की आरे खींचना चाहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा
कि हमारे मुहल्ले की सफाई नगर निगम का कोई सफाई-कर्मचारी गत दस दिनों से काम पर नहीं
आ रहा है। इस कारण आस-पास कूड़ा-कचरा डालने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं है। स्थिति
यह हो गई है कि यहाँ का वातावरण अत्यन्त दुर्गन्धमय एवं दूषित हो गया है। रोगों के
कीटाणु प्रतिदिन बढ़ रहे हैं।
अतः
हम सभी मुहल्ले वासी की सविनय प्रार्थना है कि सफाई का नियमित प्रबंध करें। आपकी ओर
से उचित कार्यवाही के लिए हम आपके आभारी रहेंगे।
धन्यवाद भवदीया
दीपक कुमार
दिनांक-20
मार्च, 2022 +2 उ०वि० गोपीकांदर
(घ) समाचार लेखन से आप क्या समझते हैं। इसकी कौन-कौन-सी विशेषताएँ हैं?
उत्तर:
"समाचार किसी भी ऐसी ताजा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक-से-अधिक
लोगों की रूचि हो और उसका अधिक-से-अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो।" लेखन द्वारा
किसी समाचारपत्र या अन्य माध्यम से जनता को इस प्रकार की सूचना देना, जागरूक और शिक्षित
बनाना तथा मनोरंजन करना समाचार लेखन होता है। पत्रकारीय लेखन का सम्बन्ध वास्तविक घटनाओं,
समस्याओं या मुद्दों से होता है। यह अनिवार्य रूप से तात्कालिकता और पाठकों की रूचियों
और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाने वाला लेखन है।
समाचार
लेखन की विशेषताएँ-
समाचार
के तत्त्व : समाचार में रोचकता, नवीनता, निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता का होना अपेक्षित
है।
विशाल
समुदाय के लिए लेखन : अखबार और पत्रिका के लिए लेखक और पत्रकारों को ध्यान में रखना
होता है कि वह ऐसे विशाल समुदाय के लिए लिख रहा है, जिसमें एक विद्वान से लेकर कम पढ़े-लिखे
मजदूर और किसान सभी शामिल हैं।
सहज,
सरल और रोचक भाषा-शैली: पाठकों के भाषा-ज्ञान के साथ-साथ उनके शैक्षिक ज्ञान और योग्यता
का विशेष ध्यान रखते हुए समाचार लेखक जटिल से जटिल एवं गूढ़ से गूढ़ विषयों को भी अत्यन्त
सहज, सरल और रोचक भाषा-शैली में लिखता है ताकि उसकी बात सबकी समझ में आसानी से आ सके।
'उलटा
पिरामिड-शैली': समाचार लेखन 'उलटा पिरामिड-शैली' में
किया
जाता है। इस शैली में किसी समाचार, घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्त्वपूर्ण तथ्य,
सूचना या जानकारी को सबसे पहले अनुच्छेद (पैराग्राफ) में लिखा जाता है। इसके बाद महत्त्व
के घटते क्रम से महत्त्वपूर्ण बातें लिखी जाती हैं।
छह
ककार : समाचार लिखते समय पत्रकार मुख्यतः छह ककारों का उत्तर देने का प्रयत्न करता
है। यह छह ककार हैं-'क्या हुआ', किसके साथ हुआ', 'कहाँ हुआ', 'कब हुआ', 'कैसे' और
'क्यों हुआ' ? किसी समाचार या घटना की रिपोर्टिंग करते समय इन छह ककारों पर ध्यान देना
आवश्यक होता है।
'इन्ट्रो'
: समाचार के 'इन्ट्रो' या 'मुखड़े' का आशय यह है कि समाचार का पहला पैराग्राफ सामान्यतः
समाचार का मुखड़ा (इन्ट्रो) कहलाता है। इसमें आरम्भ की दो-तीन पंक्तियों में सामान्यतः
तीन या चार ककारों को आधार बनाकर समाचार लिखा जाता है। यह चार ककार हैं- 'क्या, कौन,
कब और कहाँ?
समाचार
की बॉडी : समाचार के 'मुखड़े' यानी 'इन्ट्रो' को लिखने के बाद समाचार की बॉडी आर समापन
आता है जिसमें छ: में से दो शेष ककारों-'कैसे और क्यों' जबाब दिया जाता है।
खंड
- 'ग' (पाठ्यपुस्तक)
03. निम्नलिखित में से किसी एक का काव्य-सौंदर्य लिखिए- 05
(क) धूत कहौ, अवधूत कहौ, रजपूत कहौ, जोलहा कहौ कोऊ।
काहू की बेटी सों बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगारब न सोऊ।।
तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचै सो कहै कछु ओऊ।
मागि के खैबो, मसीत को सोइबो, लैबो को एक न देबको दोऊ।।
उत्तर: भक्त तुलसी वीतरागत्व वर्णित हुआ है। भाषा ब्रज
है तथा छंद सवैया है। पूरे छंद में पदमैत्री का सुंदर प्रयोग है। अनुप्रास अलंकार का
प्रयोग हुआ है। दास्य भाव की भक्ति है। 'लेने को एक न देने को दो' मुहावरे का परिवर्तित
रूप प्रयुक्त हुआ है।
(ख) अट्टालिका नहीं है रे
आतंक - भवन
सदा पंक पर ही होता
जल-विप्लव-प्लावन
क्षुद्र प्रफुल्ल-जलज से
सदा छलकता नीर
रोग-शोक में भी हँसता है
शैशव का सुकुमार शरीर।
उत्तर:
इस पद्यांश में कवि द्वारा क्रांति के दुहरे प्रभाव को रेखांकित किया गया है-शोषकों
को यह बहा ले जाती है तो शोषितों में आह्वाद भर देती है यहाँ शोषित वर्ग के प्रति गहरी
सहानुभूति है। संस्कृत शब्दों की बहुलता और भाषा की प्रतीकात्मकता से भावों की गहरी
व्यंजना हुई है। छंद-मुक्त कविता में लयात्मक सौन्दर्य है। संपूर्ण पद्यांश में अनुप्रास,
रूपक एवं अतिशयोक्ति अलंकार का प्रभाव है।
04. निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए - 03+03= 06
(क) 'विप्लव-रव से छोटे ही हैं शोभा पाते' पंक्ति में 'विप्लव-रव' से
क्या तात्पर्य है?
उत्तर:
'विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते' से आशय है कि क्रांति के आगमन में पूंजीपति वर्ग
तो बुरी तरह हिल जाता है क्योंकि इसमें उन्हें अपना विनाश दिखाई देता है। किसान मजदूर
वर्ग क्रांति के आगमन से प्रसन्नचित हो जाता है क्योंकि क्रांति का सर्वाधिक लाभ उन्हीं
को पहुँचता है।
(ख) बादलों के आगमन से प्रकृति में होनेवाले किन-किन परिवर्तनों को
'बादल राग' कविता रेखांकित करती है?
उत्तर:
बादलों के आगमन से प्रकृति में निम्नलिखित परिवर्तनों का उल्लेख कविता में हुआ है-हवा
का बहना, बादल का गरजना, मूसलधार वर्षा होना, बीज का अंकुरित होना, वज्रपात होना, छोटे
पौधों का हिलना-विकसित होना, जल-प्लावन होना, कमल की पंखुड़ियों पर जल बिन्दु का हिलना
आदि ।
(ग) शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस
का आविर्भाव क्यों कहा गया है?
उत्तर:
मेघनाद की शक्ति लगने से लक्ष्मण की मूर्छा का स्वरूप जब प्राणघातक बन गया तो सर्वत्र
करुणा रस का संचार हो गया। वैद्य सुषेण की शर्त ने इस करुण रस को अधिक प्रभावी बना
दिया जब उन्होंने सूर्योदय के पहले तक संजीवनी के लाने तथा उसी से जीवन की आशा व्यक्त
की थी। अर्द्धरात्रि बीतने के साथ ही शोक का वातावरण गहराता जा रहा था, ऐसे में सूर्योदय
के पहले ही हनुमान का संजीवनी सहित पर्वत लेकर आ जाना सबों में उत्साह भर गया । इस
तरह करुणा रस के बीच वीर रस का प्रादुर्भाव हुआ।
05. निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए - 03+03= 06
(क) नदियों का भारतीय संस्कृति में क्या महत्व है?
उत्तर:
भारतीय सभ्यता और संस्कृति में विशेष महत्त्व रहा है। हमारी संस्कृति नदियों के किनारे
ही फली-फूली है। समाज के जन्म से मरण तक जो भी संस्कार होते हैं वे नदियों के सान्निध्य
में होते हैं। नदियों के प्रति जो हमारी आस्थाएं हैं उनके मूल में कहीं-न-कहीं इनको
पोषक मानने का भाव है।
(ख) गाँव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन
पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा?
उत्तर:
गाँव में महामारी फैलने के बाद से रोग और पीड़ा तथा मृत्यु भय से लड़ने की हिम्मत लुट्टन
पहलवान की ढोलक की आवाज देती रही थी। अपने दोनों पुत्रों की मृत्यु के बावजूद उसकी
ढोलक आवाज देती रही। पहलवान जानता था कि ऐसी विषम परिस्थिति में यदि वह टूट गया तो
गाँव वालों में हिम्मत का संचार कौन करेगा?
(ग) जाति-प्रथा को श्रम-विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर
के क्या तर्क हैं?
उत्तर:
डॉ. अंबेडकर ने जाति-प्रथा को श्रम-विभाजन का एक रूपन मानते हुए कहा है कि यह श्रमिक-विभाजन
करती है। यह विभाजन मनुष्य की रुचि या क्षमता की उपेक्षा करती है। व्यक्ति के जन्म
के पहले से माता-पिता के सामाजिक स्तर का वहाँ केवल ध्यान रखकर विभाजन होता है। वह
जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बँध जाता है, उसे पेशा-परिवर्तन की आजादी नहीं मिलती।
06.बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अथवा फणीश्वरनाथ रेणु' की किन्हीं दो
रचनाओं के नाम लिखिए। 02
उत्तर:
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की दो रचनाएँ हैं-मूक नायक तथा बहिष्कार भारत।
फणीश्वरनाथ
'रेणु' की दो रचनाएँ हैं-मैला आँचल, आदिम रात्रि की महका
07. 'जूझ कहानी के शीर्षक के औचित्य पर प्रकाश डालिए। 03
उत्तर:
किसी भी रचना का शीर्षक उसके मूल कथ्य को प्रतिबिम्बित करता है। इस उपन्यास-अंश में
कथानायक आनंदा के विभिन्न स्तर पर संघर्ष को चित्रित किया गया है। कथानायक लेखक के
जुझारू व्यक्तित्व का चित्रण पूरी कथा में है। यही जुझारूपन लेखक के व्यक्तित्व की
केन्द्रीय विशेषता है। वह स्वयं व्यक्तिगत स्तर, पारिवारिक स्तर, सामाजिक स्तर, विद्यालय
में सहपाठियों के स्तर, आर्थिक स्तर-आदि सभी स्तर पर संघर्षशील दिखाई पड़ता है। उसकी
पढ़ाई की ललक एवं कुछ कर गुजरने की अभिलाषा ही उसके संघर्ष को बल देती है। अतः शीर्षक
औचित्य स्वयं सिद्ध है।
अथवा,
ऐन फ्रैंक ने अपनी डायरी में औरतों की स्थिति के विषय में विचारों की
अभिव्यक्ति कैसे की है?
उत्तर:
ऐन महिलाओं को प्रसव-पीड़ा सहने के कारण सम्माननीय मानती हैं। उनकी मान्यता है कि एक
औरत एक शिशु को जन्म देते समय जितनी पीड़ा झेलती है, उतनी पीड़ा युद्ध में लड़ने वाले
सिपाही मिलकर भी नहीं झेलते।
08. 'जूझ' पाठ के आधार पर बताइये कि लेखक किन-किन साधनों का उपयोग कविता
लेखन में करता है? 02
उत्तर:
मराठी भाषा के अध्यापक श्री सौंदलगेकर के कविता-अध्यापन ने लेखक को कविता के प्रति
रुचि जगायी। उनका सस्वर काव्यपाठ, छंद, लय, गति, अलंकार आदि का शिक्षण लेखक को कविता
समझने में सहायक होता है। स्वयं श्री सौंदलगेकर की कविता एवं अन्य कवियों के संस्मरण
से लेखक को विश्वास हुआ कि कवि किसी दूसरे लोक के नहीं, बल्कि मनुष्य ही होते हैं।
मास्टर
जी की 'मालती की बेल' कविता से लेखक को लगा कि वह भी अपने आस-पास की चीजों पर कविता
रच सकता है। पाठशाला के समारोह में गायन तथा मराठी-अध्यापक के प्रोत्साहन-शाबाशी से
लेखक में आत्मविश्वास पैदा हुआ कि वह भी कविता रच सकता है।
अथवा
ऐन फ्रैंक कौन थी? उसकी डायरी क्यों प्रसिद्ध है?
उत्तर:
ऐन फ्रैंक की डायरी विश्व की सर्वाधिक बिकनेवाली पुस्तकों में से एक है। यहूदी परिवार
की तेरह वर्षीया ऐन फ्रैंक की यह डायरी हिटलर की नाजी पार्टी के आतंक का दर्दनाक साक्षात्
अनुभव प्रस्तुत करती है । ऐन की डायरी नाजी अत्याचार की कहानी कहनेवाला जीवन्त दस्तावेज
है। यह डायरी चिट्ठी की शक्ल में है। अपनी डायरी में ऐन ने अपनी तथा साथ के लोगों की
ऊब भरी मानसिकता की चर्चा की है। बँधे और एकरस जीवन से ये लोग परेशान हैं। बातचीत के
भी सारे विषय खत्म हो चुके हैं। चुटकुले और लतीफे भी अपना अर्थ खो चुके हैं। वह युद्ध
में शामिल विभिन्न देशों की भूमिका, डच लोगों की मानसिकता आदि का वर्णन करती है।
हिटलर
यहूदियों से बेहद नफरतं करता था। वह उन्हें जर्मनी की दुर्दशा का कारण समझता था और
जर्मनी के कब्जे वाले क्षेत्रों से उनका नामों-निशान मिटाने को आतुर था। यहूदियों पर
अमानुषिक अत्याचार, ए.एस.एस से बुलावा, गैस चैंबर व फायरिंग स्क्वायड का आतंक राशन
बिजली का अभाव, ब्लैक आउट की स्थिति से गुजरना आदि अनेक तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक
परिवेश इस डायरी में चित्रित हैं । यहूदी इतिहास के जिस महत्त्वपूर्ण और कठिनाई भरे
दौर से गुजरते हुए गुप्त आवास में जीवन संघर्ष करते हैं, उसका भी सहज चित्रण ऐन की
डायरी में हुआ है है।
कुल मिला कर 'डायरी के पन्ने' पढ़कर हमें हिटलर की यातना और युद्ध की पीड़ा आदि का मार्मिक अहसास होता है।