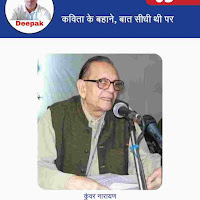3. कविता के बहाने, बात सीधी थी पर
कवि परिचय-
नाम
- कुंवर नारायण
जन्म
- 19 सितंबर सन् 1927
राज्य - उत्तर प्रदेश
काल - आधुनिक काल (समकालीन कविता)
प्रमुख रचनाएं - काव्य संग्रह चक्रव्यूह 1956
परिवेश : हम तुम, आमने-सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों
प्रबंध काव्य - आत्मजयी
समीक्षा - आज और आज से पहले
प्रमुख पुरस्कार - लगभग इन्हें हर प्रकार के पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।
1995 में कुंवर नारायण जी को कोई दूसरा नहीं काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान
किया गया था। इसके अतिरिक्त उन्हें व्यास सम्मान प्रेमचंद पुरस्कर, लोहिया सम्मान,
कबीर सम्मान आदि से भी सम्मानित किया गया।
काव्यगत विशेषताएं - कुंवर जी 1950 के आसपास लेखन की शुरुआत की। उन्होंने कहानियां, सिनेमा तथा
समीक्षाएं भी लिखें। आत्मजय जैसे प्रबंध काव्य रचना लिखकर उन्होंने एक नया उदाहरण प्रस्तुत
किया। समकालीन कविता के एक प्रमुख कवि के रूप में उन्हें जाना जाता है।
भाषा शैली - व्यर्थ की भाषा शैली से उन्होंने अपने को दूर रखा है। उनकी भाषा सरल है जो
पाठकों को पढ़ने में बोझिल नहीं लगती। खड़ी बोली के साथ-साथ उन्होंने उर्दू शब्दों
का भी प्रयोग किया है।
पाठ परिचय कविता के बहाने-कवि ने कविता के बहाने काव्य के
माध्यम से सीमा रहित विचारधारा एवं भाव प्रवाह को स्पष्ट करने की कोशिश की है। कविता
एक माध्यम हो सकता है एक देश समाज और व्यक्ति एक सूत्र में बांधने के लिए। कवि कविता
को प्रेरणादायक स्रोत के रूप में देखते हैं उनके लिए कविता राष्ट्र समाज और व्यक्ति
के निर्माण के लिए, कोमल भावनाओं को जागृत करने के लिए और मुक्त विचारधारा के लिए आवश्यक
है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उन्होंने चिड़िया, फूल और बच्चे का आश्रय लिया
है। कविता में चिड़िया की उड़ान फूलों की प्रकृति (स्वभाव) और बच्चों की छल प्रपंच
मुक्त क्रीडा को समावेशित किया है।
कविता के बहाने मूल काव्यांश एक-
कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने
कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने
बाहर भीतर
इस घर, उस घर
कविता के पंख लगा उङने के माने
चिडिया क्या जाने ?
शब्दार्थ बहाने आश्रय या सहारा देने का भाव। भीतर - अंदर।
प्रसंग - प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड में संकलित
'कविता के बहाने' नामक कविता से लिया गया है इसके रचयिता 'कुंवर नारायण' जी हैं। यह
कविता कुंवर नारायण जी की कविता संग्रह 'इन दिनों' में मूल रूप से संकलित है। 'कविता
के बहाने' में कविता के असीम संभावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने एक चिड़िया
की उड़ान का आश्रय लिया है।
व्याख्या - कवि कहते हैं कि चिड़ियों की उड़ान की एक सीमा होती है किंतु कविता की उड़ान
असीमित होती है। कविता कल्पना के रूप में उड़ान भरते हुए और सारे बंधनों को तोड़ते
हुए जनमानस तक पहुंचती है। कविता की तुलना कवि ने चिड़िया की उड़ान से की है। कवि के
अनुसार कविता की उड़ान चिड़ियों की उड़ान से अलग है। एक चिड़िया अपने निश्चित लक्ष्य
की तरफ उड़ान भरना जानती हैं किंतु कविता का लक्ष्य व्यापक होता है। चिड़िया में लगे
पंख चिड़िया को एक निश्चित सीमा तक ही उड़ने में मदद करती है किंतु कविता में लगे कल्पना
के पंख अत्यधिक ऊर्जावान होता है। बिना भेदभाव किए, बिना डरे और सीमाओं की परिभाषा
को भूलते हुए यह अपने कल्पनाओं के द्वारा मानव मन को सँवारने का काम करती है। कविता
ना केवल मन के भीतर होने वाली गतिविधियों पर लिखी जाती है अपितु कविता में निहित कल्पना
एक व्यक्ति समाज, राष्ट्र और विश्व को एक सूत्र में बांधने का काम करती है।
विशेष - प्रस्तुत काव्यांश प्रेरणादायक है।
कवि ने खड़ी बोली का प्रयोग किया है।
काव्यांश में प्रयुक्त शब्द बिल्कुल सरल है।
भाषा में क्लिष्टता का अभाव है।
कविता की उड़ान की तुलना लेखक ने चिड़ियों की उड़ान से की
है।
कविता के बहाने मूल काव्यांश दो-
कविता एक खिलना है फूलों के बहाने
कविता का खिलना भला फूल क्या जाने!
बाहर भीतर
इस घर, उस घर
बिना मुरझाए महकने के माने
फूल क्या जाने ?
कविता एक खेल है बच्चों के बहाने
बाहर भीतर
यह घर, वह घर
सब घर एक कर देने के माने
बच्चा ही जाने।
शब्दार्थ मुरझाना कुम्लाहना। महकना- खुशबू देना।
प्रसंग - प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तकमें संकलित 'कविता के बहाने' नामक कविता
से लिया गया है। इसके रचयिता कुंवर नारायण जी हैं। यह कविता कुंवर नारायण जी की कविता
संग्रह 'इन दिनों' में मूल रूप से संकलित है। उन्होंने कविता की तुलना फूलों से और
बच्चों की क्रीड़ा से की है। फूलों का खिलना एवं सुगंध फैलाना एक सीमित प्रक्रिया है
किंतु कविता से उठने वाली कल्पना रूपी गंध आजीवन समाप्त नहीं होता है। कविता बच्चों
के खेल की भांति निर्मल होती है।
व्याख्या - एक कविता को लिखते वक्त कवि के मन में सर्व हितैषी की भावना रहती है।
कविता में जो कल्पनाएं होती है वह
सर्व मंगलकारी होती है। फूलों से निकलने वाली सुंदर सुगंध मानव मन को ताजगी चमक और
शांति का एहसास कराती है किंतु एक सीमित प्रक्रिया और निश्चित अवधि के बाद यह फूल अपने
गुणों को छोड़कर मुरझा जाते हैं, किंतु कविता की कल्पनाओं से उठने वाली गंध ना तो अपनी
ताजगी और ना तो अपने चमक को छोड़ती है। यह अपनी सर्व मंगलकारी भावनाओं से मानव के लिए
उपयोगी बनी रहती है। कवि कविता को बच्चे के उस खेल की भांति मानते हैं जिसमें कोई छल
कपट प्रपंच और गंभीर उद्देश्य नहीं होत ठीक उसी प्रकार कवि भी अपने शब्दों से खेलते
हुए कल्पनाओं को सर्व मंगलकारी बना देते हैं। कविता बच्चों के खेल के भांति बिना भेदभाव
किए सारे अखिल (विश्व) को वह अपना घर मान लेता है।
विशेष - प्रस्तुत काव्यांश की भाषा खड़ी बोली है।
काव्यांश में प्रयुक्त शब्दों को प्रभावशाली तरीके से प्रयोग
किया गया है।
बाहर भीतर का अर्थ मन की आंतरिक भाव से लिया जा सकता है।
कविता में इस घर उस घर का संकेतार्थ बिना भेदभाव से है
भाषा सहज सरल और सुबोध है।
कविता में प्रश्न शैली का प्रयोग करके कवि ने काव्यांश को
सुंदर बना दिया है।
प्रश्न -अभ्यास
प्रश्न 1 - इस कविता के बहाने बताएं कि 'सब
घर एक कर देने के माने' क्या है
उत्तर - 'सब घर एक कर देने के माने' से अर्थ यह है कि बच्चे
किसी छल प्रपंच और भेदभाव के बिना खेल को खेलते हैं। खेलते वक्त उनका कोई गंभीर उद्देश्य
नहीं होता वह केवल मनोरंजन के लिए खेल को खेलते है। उनके लिए सब बराबर हैं। उसी प्रकार
कविता में कवि के द्वारा कविता में प्रयुक्त शब्दों का प्रयोग मंगलमय उद्देश्य से किया
जाता है।
प्रश्न 2 'उड़ने' और 'खिलने' का कविता से क्या
संबंध बनता है?
उत्तर - कविता में उड़ने शब्द का अभिप्राय कल्पना की उड़ान
से है। कवि कविता में कल्पनाओं के रंग भर कर कहीं भी घूम कर आ सकता है। चिड़ियों के
उड़ने की एक सीमा और ऊर्जा होती है परंतु कविता में निहित कल्पनाओं की कोई सीमा नहीं
होती है। फूलों का खिलना एवं सुगंध फैलाना एक सीमित प्रक्रिया है किंतु कविता से उठने
वाली कल्पना रूपी गंध आजीवन समाप्त नहीं होती।
प्रश्न 3 - कविता और बच्चे को समानांतर रखने
के क्या कारण हो सकते हैं?
उत्तर - कवि कविता को बच्चे के उस खेल की भांति मानते हैं
जिसमें कोई छल कपट प्रपंच और गंभीर उद्देश्य नहीं होत ठीक उसी प्रकार कवि भी अपने शब्दों
से खेलते हुए कल्पनाओं को सर्व मंगलकारी बना देते हैं। कविता बच्चों के भांति बिना
भेदभाव किए, बिना डरे और सीमाओं की परिभाषा को भूलते हुए सारे अखिल (विश्व) को अपना
घर मान लेता है।
प्रश्न 4 कविता के संदर्भ में 'बिना मुरझाए
महकने के माने' क्या है?
उत्तर - कविता के संदर्भ में 'बिना मुरझाए महकने के माने'
यह है कि फूलों से निकलने वाली सुंदर सुगंध मानव मन को ताजगी चमक और शांति का एहसास
कराती है किंतु एक निश्चित अवधि के बाद यह फूल अपने गुणों को छोड़कर मुरझा जाते हैं,
किंतु कविता की कल्पनाओं से उठने वाली गंध ना तो अपनी ताजगीऔर ना तो अपने चमक को छोड़ती
है। यह अपनी सर्व मंगलकारी भावनाओं से मानव के लिए आजीवनउपयोगी बनी रहती है।
कविता के बहाने : बहु वैकल्पिक प्रश्न उत्तर
1) 'कविता के बहाने' कविता के कवि कौन है?
क) कुंवर नारायण
ख)
आलोक धन्वा
ग)
जयशंकर प्रसाद
घ)
रघुवीर सहाय
2) 'कविता के बहाने' कविता किस प्रकार की रचना है?
क)
दोहा
ख)
चौपाई
ग) छंद मुक्त
घ)
छंद युक्त
3) कविता की तुलना किसी की गई है?
क)
फूल से
ख)
बच्चों से
ग
चिड़िया से
घ) इनमें से सभी
4) कविता के बहाने कविता में किस के अस्तित्व पर विचार किया गया है?
क) कविता के अस्तित्व पर
ख)
कहानी की अस्तित्व पर
ग) नाटक के अस्तित्व पर
घ) निबंध के अस्तित्व पर
5) कविता लिखते समय कौन-कौन से बंधन टूट जाते
हैं?
क) सीमा
ख) देश
ग) अपना-पराया
घ) इनमें से सभी
6) कवि ने किसके उड़ान को सीमित बताया है?
क) चिड़िया की
ख) धूल की
ग) हवाई जहाज की
घ) इनमें से कोई नहीं
7) 'बाहर-भीतर' में कौन सा अलंकार है?
क) उत्प्रेक्षा अलंकार
ख) उपमाअलंकार
ग) अनुप्रास अलंकार
घ) रूपक अलंकार
8) 'मुरझाए महकने के माने' में कौन सा अलंकार है?
क)
उत्प्रेक्षा अलंकार
ख)
उपमाअलंकार
ग) अनुप्रास अलंकार
घ)
रूपक अलंकार
टिप्पणी-
'म' वर्ण की आवृत्ति 2 बार से अधिक होने के कारण यहां वृत्यानुप्रास होगा। वृत्यानुप्रास
अनुप्रास अलंकार का एक भेद है।
9) बच्चों के खेलते समय कौन सा बंधन टूट जाता है?
क)
अपने-पराए
ख)
जाति
ग)
धर्म
घ) इनमें से सभी
10) कविता अपने कल्पना रूपी पंख से क्या भरती है।
क) उड़ान
ख)
निराशा
ग)
दुख
घ)
स्थिरता
11) इस घर उस घर में निहित भाव का अभिप्राय बताएं?
क) भेदभाव रहित होना
ख) भेदभाव करना
ग) निराश होना
घ) दुखी होना
12) क्या कविताएं भी भेदभाव के बंधन तोड़ा
करती हैं?
क) नहीं
ख) हां
ग) शायद नहीं
घ) इनमें से कोई नहीं
13) कविता में लगे कल्पना की उड़ान को कौन
नहीं जानता?
क) चिड़िया
ख) आदमी
ग) औरत
घ) देश
14) कविता का आजीवन ना मुरझाना कौन नहीं जानता?
क) चिड़िया
ख) आदमी
ग) फूल
घ) देश
15) बच्चे के भांति सारे भेदभाव को मिटा देना कौन जानता है?
क)
चिड़िया
ख)
आदमी
ग)
औरत
घ) कविता
16) कविता का आजीवन ना मुरझाने का क्या अर्थ है?
क) कविता का सर्वकाल उपयोगी होना
ख)
कविता का सीमित होना
ग)
कविता से किसी का भला ना होना
घ)
इनमें से कोई नहीं
17) सब घर एक कर देने का अभिप्राय है-
क) भेदभाव रहित होना
ख)
झगड़ा करना
ग)
मतभेद रखना
घ)
शांत रहना
18) खेल-खेल में कौन सब घर एक कर देते हैं?
क)
बूढ़े
ख) बच्चे
ग) जवान
घ) गांव वाले
19) कविता किसके साथ खेलता है?
क) शब्दों के साथ
ख) कलम के साथ
ग) लोगों के साथ
घ) बच्चों के साथ
20) बच्चों का खेल खेलने का उद्देश्य क्या
होता है?
क) दुश्मनी का
ख) मनोरंजन का
ग) लड़ने का
घ) इनमें से कोई नहीं
21) कवि का शब्दों के साथ खेलने का क्या उद्देश्य
हो सकता है?
क) मनोरंजन का उद्देश्य
ख) गंभीर उद्देश्य
ग) खतरनाक उद्देश्य
घ) लड़ाई का उद्देश्य
कविता के बहाने : लघु उत्तरीय प्रश्न
1. "कविता के बहाने "कविता के कवि कौन हैं और किस काव्य संग्रह
से लिया गया है?
उत्तर -कविता के बहाने कविता के कवि
हैं कुंवर नारायण जी तथा 'इन दिनों' काव्य संग्रह से यह कविता ली गई है।
2. कविता ने किस प्रकार की भाषाएं एवं छंद का प्रयोग किया गया है?
उत्तर -यह कविता छंद मुक्त है एवं
साहित्य खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है
3. कविता के बहाने बिम्ब प्रधान कविता है। कविता में कौन कौन से बिम्ब
(ईमेज, शब्द चित्र) का प्रयोग किया
गया है?
उत्तर -चिड़िया फूल एवं बच्चों का
प्रयोग बिम्म के रूप में किया गया है।
4. कविता के बहाने कविता में किस के अस्तित्व पर विचार किया गया है
और क्यों?
उत्तर -कविता के बहाने कविता के अस्तित्व
पर विचार किया गया है। आज के भागदौड़ के जीवन में लोग अपने से दूर भाग रहे हैं ऐसे
में कविता का अस्तित्व होना आवश्यक है।
5. कविता लिखते समय कौन-कौन से बंधन टूट जाते हैं?
उत्तर -कवि कविता लिखते समय सीमाओं,
देश, काल, अपने पराए के बंधन को तोड़ देता है।
6. कवि किस प्रकार से सीमा देश, काल, अपने
पराए का बंधन तोड़ता है?
उत्तर -एक कवि का मन स्वच्छ निर्मल होता है वह कविता का सृजन
केवल एक व्यक्ति के लिए, एक देश के लिए नहीं करता वह अतीत से लेकर वर्तमान सभी काल
के ऊपर लिखता है। उसके लिए सब बराबर है।
7. कविता कवि के लिए क्या है?
उत्तर -कवि के लिए कविता एक चिड़ियों की भांति उड़ान, बच्चों
की तरह भेदभाव रहित खेल, एवं ना मुरझाने वाले फूलों की महक है।
8. कविता में उड़ान, खेल, एवं महकना शब्द का
क्या अभिप्राय है?
उत्तर -कवि के लिए उड़ान शब्द का महत्व उनकी मन की कल्पना
से है एवं खेल का महत्व शब्दों के प्रयोग से है एवं महकना शब्द का प्रयोग वे अपनी रचनाओं
की उपयोगिता से करते हैं।
9. कवि ने किसके उड़ान को सीमित बताया है और
क्यों?
उत्तर -कवि ने चिड़िया की उड़ान को सीमित बताया है क्योंकि
चिड़िया के उड़ने की एक शक्ति एवं ऊर्जा होती है।
10. बाहर - भीतर में कौन सा अलंकार है?
उत्तर -बाहर भीतर में 'र' वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास
अलंकार है।
11. "चिड़िया क्या जाने" "फूल क्या जाने" में कौन
सा अलंकार है?
उत्तर -प्रश्न अलंकार।
12. बिना मुरझाए महकने के माने में कौन सा अलंकार है?
उत्तर -'म' वर्ण की आवृत्ति के कारण
अनुप्रास अलंकार है।
13. फूल और कविता दोनों महकते हैं किंतु दोनों के महकने में अंतर है
कैसे?
उत्तर -फूल निश्चित समय के बाद मुरझा
जाती है और इसकी खुशबू भी समाप्त हो जाती है किंतु कविता कालजई रचना बनकर सदियों तक
अपने अस्तित्व को बनाए रखती है।
14. बच्चों के खेलते समय कौन सा बंधन टूट जाता है?
उत्तर -बच्चों को खेलते समय अपना पराया,
धर्म जाति, सीमा आदि का बंधन टूट जाता है।
15. क्या कविताएं भी बंधन तोड़ा करती हैं?
उत्तर -कविताएं भी बंधन तोड़ा करती
हैं, क्योंकि कविताएं देश, सीमा, अपना पराया, धर्म, जाति आदि जैसे बंधनों को नहीं मानता।
16. कवि और बच्चे में क्या समानताएं हैं?
उत्तर -कवि और बच्चे दोनों निर्मल,
स्वच्छ भाव से सभी को अपनाते हैं उनके लिए कोई भी अपना पराया नहीं है।
17. एक कवि के लिए कविता लिखने का उद्देश्य
क्या हो सकता है?
उत्तर -एक कवि का कविता लिखने के कई उद्देश्य हो सकते हैं
तनाव को कम करना, मनोरंजन प्रदान करना, एकता स्थापित करना आदि जैसे कई उद्देश्य कविता
लिखने के लिए हो सकते हैं।
18. कवि
के अनुसार कविता क्या है?
उत्तर -कविता एक चिड़िया, फूल और बच्चे के खेल की भांति है।
19. कविता की उड़ान एक चिड़िया क्यों नहीं
समझ सकती है?
उत्तर -चिड़िया अपनी सुरक्षा और उद्देश्य (खाने की तलाश)
पूर्ति के लिए उड़ान भरती है किंतु कविता में लगे कल्पना के पंख से दूर वृस्तृत (विस्तार)
क्षेत्र तक ले जाती है।
20. कविता किस माध्यम से उड़ान भरती है?
उत्तर -कविता अपने कल्पना समान रूपी पंख से उड़ान भरती है।
21. कविता में बाहर भीतर किसका प्रतीक है?
उत्तर -कविता में बाहर भीतर का अर्थ मन के आंतरिक भागों में
चलने वाले गतिविधियों से है।
22. 'इस घर उस घर में' निहित भाव का अर्थ बताएं?
उत्तर -इस घर उस घर का अर्थ है भेदभाव रहित होना।
23. कविता का खिलना फूल क्यों नहीं समझ सकता?
उत्तर -कविता का खिलना फूल नहीं समझ सकता क्योंकि एक समय
के पश्चात फूल मुरझा जाते हैं और उससे उत्पन्न होने वाली खुशबू भी समाप्त हो जाती है,
किंतु कविता के द्वारा फैलाई गई विचार कभी समाप्त नहीं होती।
24. कविता एक खेल है का अर्थ बताएं?
उत्तर -जिस प्रकार बच्चे भांति-भांति के खेल अपने मनोरंजन
के लिए खेलते हैं उसी प्रकार से एक कवि भी अपने विचारों कल्पना शब्दों एवं वाक्य का
प्रयोग कविता को मनोरंजन एवं उद्देश्य पूर्ति के लिए करता है।
25. बच्चे "सब घर एक” क्यों कर देते हैं?
उत्तर -बच्चे में भेदभाव की भावना नहीं होती है इसलिए वे
सब को एक समान मानते हैं।
पाठ - बात सीधी थी पर
कवि - कुंवर नारायण
बात सीधी थी पर काव्यांश का मूल अंश- 1.
बात सीधी थी पर एक बार
भाषा के चक्कर में
ज़रा टेढ़ी फंस गई।
उसे पाने की कोशिश में
भाषा को उलटा पलटा
तोड़ा - मरोड़ा
घुमाया - फिराया
कि बात या तो बने
या फिर भाषा से बाहर आए
लेकिन इससे भाषा के साथ साथ
बात और भी पेचीदा होती चली गई।
शब्दार्थ टेढ़ी-कठिन। चक्कर फेर। कोशिश - प्रयास। पेचीदा - मुश्किल।
प्रसंग 'बात सीधी थी पर कविता के कवि 'कुंवर नारायण' जी हैं 'बात सीधी थी पर' कविता
को 'कोई दूसरा नहीं' काव्य संग्रह से लिया गया है। इस काव्यांश के द्वारा कवि कहना
चाहते हैं कि रचना का उद्देश्य पाठकों का रसास्वादन कराना है किंतु भाषा की जटिलता
अगर हो तो पाठक रचना से नहीं जुड़ पाएंगे। भाषा का प्रयोग इस प्रकार से होनी चाहिए
कि पाठक उस रचना के साथ अपने आप को जोड़ सके।
व्याख्या - कवि अपने मन के अंदर उठने वाले द्वंद को कविता के माध्यम से व्यक्त किया
है। वे स्वीकार करते हैं कि एक सरल सी बात को उन्होंने भाषा के बढ़िया प्रयोग करने
के चक्कर में जटिल बना दिया। कविता के सही अर्थ प्राप्त करने के प्रयत्न में बात और
भी मुश्किल होती चली गई क्योंकि शब्दों के जाल और भी घने होते चले गए। प्रस्तुत पद्यांश
में कवि ने ऐसे साहित्यकारों पर व्यंग किया है जो अपने भाषाई प्रभाव जमाने के चक्कर
मेंसाहित्य को इतने कठिन बना देते हैं कि पाठक उसके अर्थ को समझने में असमर्थ हो जाते
हैं।
विशेष - काव्यांश में साहित्य खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है।
कवि भाषा के फेर में पड़ने से बचने का संदेश देना चाहते हैं।
कवि का मानना है कि कोई भी रचना पाठकों के लिए की जाती है
अपने पांडित्य प्रदर्शन के लिए नहीं।
उल्टा-पुल्टा, तोड़ा-मरोड़ा, घुमाया-फिराया में अनुप्रास
अलंकार है।
साथ-साथ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है।
कविता की भाषा सहज सरल और मुहावरों से युक्त है
काव्यांश प्रेरणादायक है।
बात सीधी थी पर काव्यांश का मूल अंश दो-
सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना
मैं पेंच को खोलने के बजाए
उसे बेतरह कसता चला जा रहा था
क्यों कि इस करतब पर मुझे
साफ़ सुनाई दे रही थी
तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे
डर था ज़ोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई
और वह भाषा में बेकार घूमने लगी।
शब्दार्थ - मुश्किल - कठिन। पेंच किसी दो वस्तु को जोड़ने का मशीनी उपाय। बजाए - बदले में। बेतरह बुरी
तरह से। करतब तमाशा। तमाशबीन दर्शक (देखने वाला)। कसाव तनाव, खिंचाव। आखिरकार अन्नतहा।
जोर-जबरदस्ती - बलपूर्वक किया गया काम। चूड़ी - कलपुर्जा में बनाई गई गोल संरचना में
बनाई गई रेखा।
प्रसंग - 'बात सीधी थी पर' कविता के कवि 'कुंवर नारायण' जी हैं। 'बात सीधी थी पर' कविता
को 'कोई दूसरा नहीं' काव्य संग्रह से लिया गया है। इस काव्यांश के द्वारा कवि कहना
चाहते हैं कि बात को सरल ढंग से अभिव्यक्त करने का प्रयास करना चाहिए ताकि अभिव्यक्ति
में जटिलता ना आ पाए, किंतु रचनाकार मूल समस्या को समझने पर ध्यान ना देकर वाहवाही
लूटने का प्रयास करें तो उसकी रचना जनहित के लिए नहीं हो सकती।
व्याख्या - इस पद्यांश में कवि कहना चाहते हैं कि एक रचनाकार को धैर्य पूर्वक अभिव्यक्ति करनी चाहिए और
वह अभिव्यक्ति सरल शब्दों में ही होनी चाहिए ताकि बात को समझने में कोई उलझन ना हो।
कवि घुमावदार शब्दों को करतब की संज्ञा दी है। व्यक्ति अगर जबरदस्ती भाषाई धौंस जमाने
के लिए शब्दों को रचना में ठुसता चला जाए तो रचना सामान्य पाठकों के किसी काम की नहीं
रह जाती यह केवल तमाशबीनों की वाहवाही ही लूट पाती है और इस प्रकार शब्दों की मर्यादा
भी समाप्त हो जाती है।
विशेष काव्यांश में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है।
कविता की भाषा सहज व सरल है।
कविता में उर्दू का तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है।
साफ सुनाई जोर-जबर्दस्ती में अनुप्रास अलंकार है।
तमाशबीन और करतब शब्दों में व्यंग का भाव छिपा है।
कवि रचना में अभिव्यक्ति को सरल शब्दों से प्रकट करने का
संदेश देना चाहते हैं।
'बात सीधी थी पर' काव्यांश का मूल अंश- 3
हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोंक दिया। ऊपर से ठीकठाक
पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकता मुझसे खेल रही थी,
बात ने, जो एक शरारती बच्चे की तरह
मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा-
"क्या तुमने भाषा को
सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा?"
शब्दार्थ - ताकत - शक्ति। शरारत बदमाशी। सहूलियत आसानी सुगमता सुविधा। बरतना - व्यवहार
करना।
प्रसंग - 'बात सीधी थी पर' कविता के कवि 'कुंवर नारायण' जी हैं 'बात सीधी थी पर' कविता
को 'कोई दूसरा नहीं' काव्य संग्रह से लिया गया है। इस काव्यांश के द्वारा कवि सटीक
अभिव्यक्ति के लिए उचित भाषा के चुनाव पर बल देना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि ऐसी शब्दों
का प्रयोग किस काम का जब रचना प्रभावहीन ही हो जाए।
व्याख्या कवि अपने द्वंद को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि भाषा के साथ जबरदस्ती करने
का परिणाम वही हुआ जिसका डर उन्हें था, रचना की मर्यादा ही टूट गई। बात की कसावट अगर
समाप्त हो जाए तो रचना प्रभावहीन लगती है। रचना को प्रभावहीन जानकर कवि को ऐसा प्रतीत
हो रहा था मानो भाषा उसे चेता रही हो कि भाषा अभिव्यक्ति का एक माध्यम है इसे कील की
तरह जबरदस्ती रचना में ठोका नहीं जा सकता । भाव के अनुसार शब्दों का चयन न कर पाने
के कारण लेखक को परेशानी का सामना करना पड़ता है और उन्हें एहसास होता है उनकी रचना
में कसावट नहीं बची है अर्थात् उनकी रचना प्रभावहीन हो गई है।
विशेष कविता की भाषा खड़ी बोली है।
भाषा में तत्सम तथा उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है।
भाषा बिम्ब प्रधान है।
'पसीना पोछना' में मुहावरे का प्रयोग किया गया है।
'कील की तरह ठोकना 'में उपमा अलंकार है।
कवि ने काव्यांश में बात का मानवीकरण किया है।
प्रश्न -अभ्यास
प्रश्न 1 - 'भाषा को सहूलियत' से बरतने से
क्या अभिप्राय है
उत्तर -भाषा को सहूलियत से बरतने का अभिप्राय यह है कि रचना
में भाव के अनुसार भाषा को चुनना और उसका प्रयोग करना चाहिए अन्यथा भाषा की जटिलता
में रचना प्रभावहीन हो जाता है।
प्रश्न 2 - बात और भाषा परस्पर जुड़े होते
हैं, किंतु कभी-कभी भाषा के चक्कर में 'सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है' कैसे?
उत्तर - बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं क्योंकि हम अपनी
बात को समझाने के लिए हम किस प्रकार के भाषा का प्रयोग कर रहे हैं यह देखना आवश्यक
है। कई बार हम लोग सीधी सी बात कहने के लिए इतनी कठिन भाषा का प्रयोग कर लेते हैं कि
वह वाक्य अपना अर्थ ही खो देता है।
बात सीधी थी पर : लघु उत्तरीय प्रश्न
1. 'बात सीधी थी पर' कविता के कवि कौन है एवं किस काव्य संग्रह से यह
कविता ली गई है?
उत्तर -बात सीधी थी पर कवि 'कुंवर
नारायण' जी द्वारा लिखी गई कविता है एवं यह 'कोई दूसरा नहीं 'काव्य संग्रह से लिया
गया है
2. 'बात सीधी थी पर' कविता में किस पर विशेष जोर दिया गया है?
उत्तर -भाषा को सरल शब्दों में कहने
पर जोड़ दिया गया है।
3. 'बात सीधी थी पर' कविता में किस प्रकार की भाषा शैली एवं अलंकार
का प्रयोग किया गया है?
उत्तर -बात सीधी थी पर कविता मुक्त,
छंद संरचना है एवं इसमें साहित्य खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है।
4. सीधी सी बात किस के चक्कर में फंस गई?
उत्तर -भाषा के चक्कर में सीधी सी
बात फंस गई।
5. सीधी सी बात भाषा के चक्कर में क्यों फंस गई?
उत्तर -भाषा का चमत्कारिक प्रदर्शन
के कारण सीधी सी बात भाषा के चक्कर में फंस गई।
6. बात को सही करने के लिए कवि ने क्या-क्या किया?
उत्तर -बात को सही करने के लिए कवि
ने भाषा को तोड़ा-मरोड़ा, घुमाया-फिराया।
7. बात को प्रभावशाली बनाने के चक्कर में कवि
ने कविता में क्या किया?
उत्तर -कविता के शब्दों में थोड़ा बदलाव किया।
8. कविता में शब्दों के बदलाव करने पर क्या
कविता प्रभावशाली बन पाई?
उत्तर -नहीं कविता की भाषा और भी कठिन हो गई।
9. कवि किसे पाने की कोशिश करता है?
उत्तर -कवि बात (वाक्य, कथन) को पाना चाहता है।
10. भाषा
के साथ साथ बात कैसी हो गई?
उत्तर -भाषा के साथ-साथ बात और भी पेचीदा (कठिन) हो गई।
11. किन
कारणों से बात पहले से अधिक पेचीदा हो गई?
उत्तर -बिना धैर्य से समझे, शब्दों को उल्टा-पुल्टा करने,
तोड़ने-मरोड़ने, घुमाने-फिराने से भाषा और भी पेचीदा हो गई।
12. उल्टा-पुल्टा, तोड़ा-मरोड़ा, घुमाया-फिराया
में कौन सा अलंकार है?
उत्तर -अनुप्रास अलंकार है।
13. पेंच खोलने का अर्थ बताएं?
उत्तर -बात को ठीक करना।
14. कवि बात को किस तरह से कसते जा रहे थे?
उत्तर -कवि बात को बेतरह (बुरी तरह से) कसते जा रहे थे।
15. कवि
को किस बात पर शाबाशी मिल रही थी?
उत्तर -भाषा के शक्ति प्रदर्शन पर उन्हें वह शाबाशी मिल रही
थी।
16. कविता
के साथ आखिरकार क्या हुआ?
उत्तर -क्लिष्ट शब्दों, मुहावरों पर्यायवाची आदि के प्रयोग
करने से सीधे-साधे, सरल कविता का अर्थ बदल गया।
17. बात की चूड़ी मर गई का अर्थ बताएं?
उत्तर -बात का प्रभावहीन हो जाना।
18. दो
वस्तुओं को जोड़ने के लिए किस की आवश्यकता होती है?
उत्तर -दो वस्तुओं को जोड़ने के लिए पेंच की आवश्यकता पड़ती
है।
19. चूड़ी भाषा में बेकार क्यों घूमने लगी?
उत्तर -प्रत्येक भावको समझाने के लिए एक निश्चित भाषा का
प्रयोग किया जाता है किंतु जब हम अपने भाव को समझाने के लिए भाषा में अधिक प्रयोग करने
लगते हैं तो बात या कथन भाषा में बेकार घूमने लगती है।
20. पेंच
को कसने के लिए क्या आवश्यक है?
उत्तर -पेंच को सही दिशा में घुमाना चाहिए ताकि पेंच वस्तुओं
पर अपनी पकड़ मजबूती से बनाए रखें।
21. अपनी झूठी तारीफ सुनकर कवि को क्या महसूस
हो रहा था?
उत्तर -कवि खुशी का अनुभव कर रहे थे और इसी चक्कर में भाषा
(भावको बताने का माध्यम) को और भी कठिन करते जा रहे थे।
22. भाषा
के सही प्रयोग न कर पाने के कारण कवि ने अंत में क्या किया?
उत्तर -थक हार कर उन्होंने भाषा को कील की तरह बात पर ठोक
दिया।
23. कील
का अर्थ बताएं?
उत्तर -लोहे का पतला, लम्बा एवं नुकीला टुकड़ा।
24. ठोकने
का अर्थ बताएं?
उत्तर -किसी भी वस्तु को बलपूर्वक लगाना ठोकने की प्रक्रिया
कहलाती है।
25. कील
ठोकने से बात (वाक्य या कथन) की स्थिति क्या हो गई?
उत्तर -बात में ना तो कसाब रहा ना ताकत। अर्थात बात प्रभावहीन
हो गई।
26. कवि
के साथ कौन खेल रहा था?
उत्तर -कवि के साथ बात शरारती बच्चे की भांति खेल रहा था।
27. कविता
में शरारती बच्चे के साथ बात की तुलना क्यों की गई है?
उत्तर -ऐसे बच्चे जो संभाल में ना आए उन्हें शरारती बच्चे
कहां जाता है कवि कविता में बात को संभाल नहीं पा रहे थे इसलिए बात को शरारती बच्चे
की संज्ञा दी गई है।
28. कवि को पसीना क्यों आ गया?
उत्तर -कविता में सही बात का प्रयोग ना कर पाने के कारण कवि
को पसीना आ गया।
29. 'भाषा
को सहूलियत से बरतने' का क्या अर्थ है?
उत्तर -'भाषा का सहूलियत से बरतने' का अर्थ है भाषा का प्रयोग
आसान शब्दों में करना अधिक से अधिक लोग बात को समझ पाए।
30. बात ने, जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे
खेल रही थी मैं कौन सा अलंकार है?
उत्तर -मानवीय अलंकार। इस पंक्ति में बात को शरारती बच्चे
की तरह माना गया है इसलिए यहां पर बात का मानवीकरण हो गया है।
31. बात
की पेंच खोलने का अर्थ बताएं?
उत्तर -बात में कसावट का ना होना।
32. बात
का शरारती बच्चे की तरह खेलना का क्या अर्थ है?
उत्तर -बात का पकड़ में ना आना।
बात सीधी थी पर : बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर
1) 'बात सीधी थी पर' कविता के कवि कौन है?
क) कुंवर नारायण
ख)
रघुवीर सहाय
ग)
महादेवी वर्मा
घ)
जयशंकर प्रसाद
2) 'बात सीधी थी पर' कविता किस प्रकार की रचना है?
क)
दोहा
ख)
चौपाई
ग) छंद मुक्त
घ)
छंद युक्त
3) 'बात सीधी थी पर' कविता में किस पर विशेष जोर दिया गया है?
क) सरल भाषा पर
ख)
जटिल भाषा पर
ग)
सरल एवं जटिल दोनों भाषा पर
घ)
इनमें से कोई नहीं
4) सीधी सी बात किस के चक्कर में फंस गई?
क)
सरल भाषा के चक्कर में
ख) जटिल भाषा के चक्कर में
ग)
मधुर भाषा के चक्कर में
घ)
कठोर भाषा के चक्कर में
5) भाषा का चमत्कारिक प्रदर्शन के कारण सीधी सी बात क्या बन जाती है?
क) जटिल
ख)
सरल
ग)
मधुर
घ)
कठोर
6) 'साथ- साथ' में कौन सा अलंकार है?
क)
उत्प्रेक्षा अलंकार
ख)
अनुप्रास अलंकार
ग) पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार
घ)
रूपक अलंकार
7) उलटा-पुलटा, तोड़ा-मरोड़ा घुमाया- फिराया में कौन सा अलंकार है?
क)
उत्प्रेक्षा अलंकार
ख) अनुप्रास अलंकार
ग)
अतिशयोक्ति अलंकार
घ)
रूपक अलंकार
टिप्पणी
उपरोक्त दिए गए उदाहरण में शब्दों के अंतिम अक्षर (टा, ड़ा, या) एक समान या एक तुक
होने के कारण यहां पर अन्त्यानुप्रास अंलकार होगा। अन्त्यानुप्रास अनुप्रास अलंकार
का एक भेद है।
8) कवि बात को किस तरह से कसते जा रहे थे?
क) बेतरह (बुरी तरह से)
ख)
अच्छी तरह से
ग)
धैर्य के साथ
घ)
इनमें से कोई नहीं
9) धैर्य से समझे बिना, शब्दों को उल्ट- पुल्टा करने, तोड़ने-मरोड़ने,
घुमाने- फिराने से भाषा क्या हो गई।
क)
समझने लायक
ख)
सरल
ग) पेचीदा
घ)
आसान
10) कवि को किस बात पर शाबाशी मिल रही थी?
क) भाषा के चमत्कारिक प्रदर्शन पर
ख)
सरल भाषा पर
ग)
मधुर भाषा पर
घ)
शब्दों के प्रयोग पर
11) भाषा का क्या करने से बात और अधिक पेचीदा हो गई?
क)
तोड़ने-मरोड़ने
ख)
उलटने-पलटने
ग) घुमाने-फिराने
घ) उपर्युक्त सभी
12) भाषा की जटिलता से कविता के साथ आखिरकार
क्या हुआ?
क) अर्थ बदल गया
ख) अर्थ सरल हो गया
ग) अर्थ मधुर हो क्या
घ) इनमें से सभी
13) बात कवि के साथ किसके समान खेल रही थी?
क) बच्चे के समान
ख) खिलाड़ी के समान
ग) जोकड़ के समान
घ) इनमें से कोई नहीं
14) 'बात ने, जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे
खेल रही थी' में कौन सा अलंकार है?
क) मानवीय अलंकार
ख) अनुप्रास अलंकार
ग) उपमा अलंकार
घ) रूपक अलंकार
15) ठीक-ठाक, पसीना पोंछने मैं कौन सा अलंकार है?
क)
उत्प्रेक्षा अलंकार
ख) अनुप्रास अलंकार
ग)
अतिशयोक्ति अलंकार
घ)
रूपक अलंकार
16) 'पेंच खोलने' का अभिप्राय बताएं?
क)
बात को जटिल करना
ख) बात को ठीक करना।
ग)
बात को प्रभावहीन करना
घ)
बात को उलझाना
17) 'साफ सुनाई', 'जोर-जबरदस्ती' में कौन सा अलंकार है?
क)
उत्प्रेक्षा अलंकार
ख) अनुप्रास अलंकार
ग)
अतिशयोक्ति अलंकार
घ)
रूपक अलंकार
18) 'भाषा को सहूलियत' से बरतने से क्या अभिप्राय है?
क) भाषा का आसान व्यवहार
ख)
भाषा का कठिन प्रयोग
ग)
भाषा का कठोर प्रयोग
घ)
इनमें से कोई नहीं
19) 'कील की तरह ठोकना' में कौन सा अलंकार है?
क)
उत्प्रेक्षा अलंकार
ख)
अनुप्रास अलंकार
ग) उपमा अलंकार
घ)
रूपक अलंकार
20) तमाशबीन और करतब शब्दों में कौन सा भाव छिपा हुआ है?
क) व्यंग का
ख)
हंसी का
ग)
विनोद का
घ)
दुख का
21) बात को सही तरीके से प्रयोग ना करने के कारण लेखक को क्या आ गया?
क)
हंसी
ख)
गुस्सा
ग) पसीना
घ)
आंसू
22) पसीना पोंछने का क्या अभिप्राय है?
क) कठिनाई का अनुभव करना
ख)
आसान लगना
ग)
उचित लगना
घ)
उत्तम लगना
23) जोर जबरदस्ती भाषा के प्रयोग से आखिरकार क्या हुआ?
क)
बात प्रभावशाली नहीं रही
ख)
बात में कसावट नहीं रहा
ग)
अर्थ में परिवर्तन हो गया
घ) इनमें से सभी
24) बात की सीधी ना होने पर कवि ने हार कर क्या किया?
क)
बात को सुलझाने की कोशिश की
ख) बात को ऐसे ही छोड़ दिया
ग)
बात में सरलता ला दी
घ)
इनमें से कोई नहीं